अशोक तिवारी
शिक्षा - पी-एच.डी.(हिंदी), एम.ए(हिंदी), एम.एस.सी.(गणित), बी.एड.
लेखन विधाएं: कविता, कहानी, रेखाचित्र एवं लेख
कृतियां
ऽ सुभाषचंद्र बोस और आज़ाद हिंद फ़ौज (दो भागों में)
ऽ सुनो अदीब (कविता संग्रह)
ऽ धार काफ़ी है (संपादन-जनकवि शील पर केंद्रित)
ऽ मुमकिन है (कविता संग्रह)
ऽ सरकश अफ़सानेः जनम के चुनींदा नुक्कड़ नाटक (संपादन)
ऽ समकालीन हिंदी कविता और सांप्रदायिकता (शीघ्र प्रकाश्य)
थियेटर-
ऽ 1987 से अभिनय व निर्देशन
ऽ 1991 से जन नाट्य मंच के साथ लगातार नाट्यकर्म
पत्रिका - नुक्कड़ जनम संवाद (त्रैमासिक थियेटर पत्रिका) के संपादन में 18 सालों से लगातार सक्रिय
पुरस्कार :
ऽ वर्तमान साहित्य मलखान सिंह सिसौदिया कविता पुरस्कार - 2007
(सुनो अदीब किताब पर)
सीखने की ज़रूरत
जिन सवालों को विजेंद्र जी ने ‘पहली बार’ के पोस्ट लेख ‘आज की आलोचना का गिरता स्तर’ में उठाया है, वे अहम हैं। ध्यान से देखें तो ये कुछ उन अप्रासंगिक सवालों को उठाए जाने की मुख़ालफत में उठे हैं जिन्हें प्रोफ़ेसर मार्का कुछ कथित विद्वान उठा रहे हैं। समकालीन कविता का पूरा परिदृश्य दरअसल 60-70 के दशक को पढ़े या समझे बग़ैर नहीं जाना जा सकता। यह सच है कि प्रगतिशील कविता के बरक्स नई कविता खड़ी हुई। बरक्स कहने का यहां मतलब आपने-सामने होना नहीं है बल्कि कविता के अंदर आम इंसान को जगह मिलने की क़वायद के खि़लाफ़ कविता में बाजीगरी पैदा करना एवं उसके शिल्प में आकर्षण पैदा करना रहा।
हम जानते हैं कि ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ और ‘इप्टा’ का हिंदुस्तान की आज़ादी में उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह योगदान इतिहास में महज़ दर्ज होने की गरज से नहीं था बल्कि उसी इतिहास में सामान्य आदमी की भूमिका को सुनिश्चित करने के बारे में भी था। इनकी विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दूर-दराज के इलाक़ों में की जाती थीं। अस्थाई मंच बनाकर नाटक, प्रहसन आदि खेले जाते जिनके विषय आम जनता और उनकी तकलीफ़ों से जुड़े होते। विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियों के साथ-साथ तमाम तरह के गीत, नज़्म, ग़ज़ल एवं कविताएं इत्यादि उन्हीं लोगों के बीच में प्रस्तुत की जातीं। कहने का आशय यह है कि आम इंसान को केंद्र में लाने की सुगुबगाहट शुरू हो चुकी थी। जो यक़ीनन रूस के माक्र्सवादी मॉडल का प्रभाव था जो दुनिया भर में तेज़ी से फैला था। बड़े-बड़े रचनाकारों को देखिए क्या लिख रहे थे। निराला ‘कुकुरमुत्ता’ से लेकर ‘नए पत्ते’, नागार्जुन कविता में अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करते हुए अपने रचनाकर्म को आगे बढ़ा रहे थे। केदारनाथ अग्रवाल एवं शील आदि के साथ राजीव सक्सैना ...धू धू कर जल रहा समाज...सरीखी कविताएं लिख रहे थे। ऐसे में कुछ हस्ताक्षर ऐसे भी थे जो प्रगतिवादी स्वर को कमज़ोर बनाने के भरसक प्रयास कर रहे थे। अज्ञेय उन्हीं कवियों की पंक्ति में आगे खड़े थे जो अमरीकी प्रभाव में आकर साहित्य में व्यक्तिवादी रुझान को बढ़ावा देने में लगे थे। तार-सप्तक के वजूद में आने के लिए अज्ञेय की छटपटाहट भी देखी जा सकती है। प्रगतिशील धारा के कई कवि इसमें शामिल रहे - यह सच है - मगर यह संग्रह अपनी ख्याति के कौन से आयाम तय करके गया? ये एक बड़ा सवाल है। हमें याद होगा नई कविता का नारा भी ‘new poetry’ की तरज पर ही था।
हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क की संरचना में आया बदलाव असंतोषजनक था। यह असंतोष छठवें दशक में किसी न किसी रूप में साहित्य का हिस्सा बना। उससे भी ज़्यादा आम इंसान उस सपने के पूरे होने के इंतज़ार में रहा जो देश के बेहतर भविष्य के रूप में देखे गए थे। ‘बॅटवारे’ का घाव इतना गहरा था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। कविता में एक शून्य-सा था जो छठवें दशक के बीच पसरा था। हालांकि इस शून्य को तोड़ते हुए कई सुर अपने अंदाज़ में रचनाकर्म में लगे थे। मुक्तिबोध की कविता का बिंब विधान इसी दौर की उपज था। निराला, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगलसिंह सुमन, शील, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि के साथ साथ शंकर शैलेंद्र, कैफ़ी आज़मी, साहिर लुधियानवी आदि बहुतेरे कवि एवं शायर इस दौर की धड़कन के साथ एकात्म होते हुए विभिन्न बदलावों को रेखांकित कर रहे थे। राजनीतिक उठापटक एवं अदूरदर्शी नीतियों ने लोगों के अंदर हताशा व निराशा भर दी थी जो राजकमल चैधरी धूमिल, श्रीकांत वर्मा आदि के लेखन में साफ़तौर पर नज़र आ रही थी। अकविता, भूखी पीढ़ी, बीट कविता आदि का पूरा परिदृश्य इसी दौर की उपज था।
यह दौर वह था जब कविता की ही नहीं साहित्य की भी एक दिशा तय हो रही थी। सातवां दशक आंदोलन के स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण दशक के रूप में याद किया जाता है। इस दौर में कविता के तमाम रुझान भी देखे जा सकते हैं। इन रुझानों को प्रकट करते हुए केदारनाथ अग्रवाल, शील, नागार्जुन, त्रिलोचन एवं विजेंद्र आदि कवि पूरी ईमानदारी के साथ कविकर्म में जुटे थे। हमें याद होगा, ये वही दौर था जब नागार्जुन घोर सांप्रदायिक बाल ठाकरे को अपनी कविता में जवाब देते हुए सभी सांप्रदायिक शक्तियों की अच्छे से ख़बर ले रहे थे।
इसी दशक में जनवादी कविता की चेतना का विरोध भी चरम पर रहा। धर्मवीर भारती और विजयदेव नारायण साहू आदि ‘परिमल समूह’ के तहत मार्क्सवादी चेतना पर सीधे-सीधे हमला कर रहे थे। इसके चलते बहुत-सी ऊल-जलूल प्रतिस्थापनाएं तक करने की कोशिश की गईं। ये हमला एकाएक हुआ हो, ऐसा भी नहीं था। इस तरह के हमले हमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ, जो कदाचित महान लेखक मैक्सिम गोर्की के ‘तय करो किस ओर हो तुम’ के फलस्वरूप बना, देखने को मिलने लगे। तीखे वैचारिक संघर्ष होते रहे। शिवदान सिंह चैहान, चंद्रबली सिंह, रामविलास शर्मा एवं प्रकाशचंद्र गुप्त आदि तमाम माक्र्सवादी आलोचक विरोधीधारा के तर्कों से रूबरू होते रहे।
अब अगर ‘वागर्थ’ पत्रिका ‘80’ के बाद की कविता पर अपने को केंद्रित करती है, तो इसके निहतार्थ क्या हैं, इसे समझना होगा। विजेंद्रजी का यह सवाल कि ‘80’ के बाद की कविता क्यों, 70 के बाद की कविता से चर्चा क्यों नहीं, एक ख़ास रुझान की ओर इशारा है। विजेंद्रजी की इस टिप्प्णी से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि 70 के बाद के दशकों का भी जब अध्ययन किया जाएगा तो निःसंदेह 70 से 80 के बीच का दौर एक ऐसा दौर रहा है जो न केवल कविता के लिए, बल्कि कला, साहित्य एवं संस्कृति के साथ-साथ मानवीय एवं राजनीतिक सरोकारों को भी प्रभावित करता है। यह दौर बेहद उथल-पुथल का रहा है। एक ओर जहां 60-70 का दौर बेहद असमंजस, दुविधा एवं संकटग्रस्त रहा है; वहीं 70-80 के दौर में राजनीतिक उठा-पटक के साथ-साथ फ़ासीवादी तेवरों का इमरजेंसी में लागू होना, बोलने के अधिकार एवं संप्रेषणीयता पर अंकुश का बड़ा भारी कलंक रहा है। अब उस दौर को भुलाकर सिर्फ 80 के बाद की कविता पर बात करना और ख़ासकर उन लोगों की बात करना जो रूपवाद के साथ-साथ कविता की वापसी का नारा देते रहे।
यह सोचने की बात है कि ये कौन लोग हैं जो कविता की वापसी का नारा देते हैं और जिनका मानना है कि कविता की मौत हो गई है। कौन लोग हैं जिन्हें 60-70 और 70-80 के बीच की कविता कविता नज़र नहीं आती और एकाएक 80 के बाद के दौर में कविता में उन्हें मार्के की चीज़ नज़र आने लगती हैं...सोचने का विषय है।
मुझे लगता है प्रमुख सवाल विचारधारा का है। हम जानते हैं 80 के बाद कविता के क्षेत्र में कोई विशेष मोड़ नहीं आए। फिर बार-बार उसी बात को उठाते हुए कुछ चुनींदा संदर्भो और चुनींदा कवियों या लेखकों को लेकर अपनी बात को पुष्ट करते रहना एक ख़ास रुझान की ओर इशारा तो करता ही है, बल्कि 80 के बाद की कविता में से कई बार कवितापन भी ग़ायब होता नज़र आया है। कविता का समाज साक्षेप नज़रिया आत्मकेंद्रित होकर रह गया। अब ऐसे में आत्मकेंद्रित होते चले जाते अशोक बाजपेई और कुंवर नारायण जैसे कवि न केवल एक बड़े कवि के रूप में ख्याति प्राप्त करने की होड़ में लगे रहते हैं बल्कि बड़े कवियों(वास्तविक) की उपेक्षा करते हुए उन्हें हाशिए पर डाल देते हैं। ऐसा कौन करता है और क्यों? इस पर विजेंद्र जी की एक टिप्पणी उल्लेखनीय है - ”हिंदी आलोचना का गिरता स्तर वाकई शोचनीय है। समीक्षक को कविता में यथार्थ की छाया प्रतीति को भेदकर उसके सार तक जाना ज़रूरी है। मेरा अपना अनुभव है कि अधिसंख्य समीक्षक अपनी सुविधा के लिए कुछ ऐसी पंक्तियां चुन लेते हैं जिनसे वे अपनी बात प्रमाणित कर सकें। इससे कविता के सार तक नहीं पहुंचा जा सकता। कविता के सार तक पहुंचने के लिए आलोचक को बड़ा श्रम करना पड़ता है। वैसा धैर्य, वैसी साधना आज के हिंदी समीक्षकों में विरल है। हमारे यहां आलोचक को कवि का मित्र, स्वामी, मंत्री, शिष्य और गुरु तक कहा है - यानी उसके और कवि के रिश्ते बड़े व्यापक होते हैं।“ (विजेंद्रजी का साक्षात्कार - ‘साहित्य: शिवेतर क्षतये’ अलाव, अंक-35)
पिछली शताब्दी में मार्क्सवाद का व्यावहारिक रूप दुनिया में बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर साकार होते देखा गया। मेहनतकश और किसानों की भूमिका को सुनिश्चित करते हुए कई देशों सरकारें इसी के अनुरूप ढलीं। पूंजीवाद के शिकंजे को चुनौती देने वाला साम्यवादी ढांचा अपने पूरे रंग-ढंग के साथ व असरदार तरीक़े से सामने आया। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि उन्हीं देशों में ऐसे लोग भी बराबर बने रहे जिन्होंने साम्यवाद को दिलो-दिमाग़ से स्वीकार नहीं किया और वे जाने-अनजाने पूंजीवादी रवैयों का समर्थन करते रहे। दोनों विचारधाराओं का द्वंद्व यक़ीनन नया नहीं है। साम्यवाद जहां एक ओर इंसान की प्रगति एवं वैज्ञानिक आधार का हामी रहा है, वहीं दूसरी ओर पूंजीवाद पूंजी को सर्वोपरि मानकर हर चीज़ को उसी के अनुरूप देखता है। साम्यवादी व्यवस्था जहां इंसान के इंसान बने रहने व इंसानियत को कु़दरत का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा मानती है, वहीं पूंजीवादी व्यवस्था में सभी रिश्ते, क़ायदे-क़ानून आदि पूंजी से ही तय होते हैं। साम्यवादी व्यवस्था जहां एक ओर समाज के हर तबक़े की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए समानता के व्यवहार पर ज़ोर देती है जबकि दूसरी व्यवस्था चंद मुट्ठीभर लोगों की वह व्यवस्था होती है जो बाक़ी लोगों पर थोपी जाती है। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत चेतना का आधार वैज्ञानिक हो ही हो - यह ज़रूरी नहीं। बल्कि इसी व्यवस्था की देन बाज़ारवाद है जिसके चलते हर तरह के तीज-त्यौहार आदि तय होते हैं। पूंजी के खेल का असली अखाड़ा ही तो है बाज़ार। पूंजी का असमान वितरण बाज़ारवाद की पहली और ज़रूरी शर्त है। बाज़ारवाद के हथकंडों का हमेशा से ही प्रगतिशील चेतना विरोध करती रही है।
साहित्य में बाज़ारवाद के सरोकारों को निभाने वाले भी कम नहीं रहे हैं, बल्कि पिछले दो दशकों में ख़ासकर 1991 के बाद जब उदारीकरण की नीति के तहत बाज़ार की खुली नीति लागू की गई, उसका प्रभाव खूब फूला फला है। हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का बाज़ार खूब गर्म रहा है। पत्रिकाओं में लगने वाली पूंजी का असर भी साफ़ परिलक्षित होता है। नया ज्ञानोदय, वागर्थ जैसी पत्रिकाएं किन मूल्यों का प्रतिपादन करने पर तुली हैं - यह भी देखने की चीज़ है। हंस, कथादेश, कथन आदि पत्रिकाएं साहित्यिक सरोकारों के नाम पर जो कुछ भी परोस रहीं है उसमें आमजन कितना है - यह सोचने का विषय है। लगभग ग़ायब। इसके कारण क्या हैं? जाने-अनजाने कहीं ये सभी पत्रिकाएं पूंजीवाद के उन्हीं हथकंडों की शिकार तो नहीं हो रहीं हैं जिनका विरोध करने के लिए एक ज़माने में वो खड़ी हुई थीं। जिनमें कई बार फूहड़ एवं अश्लील जुमलेबाज़ी के चलते सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की गई है (नया ज्ञानोदय के पिछले दिनों के कई कांड तो अभी लोगों की ज़हन में ताज़ा होंगे।) इसी के साथ-साथ विभिन्न सरकारी पत्रिकाएं- साक्षात्कार, मधुमती, भाषा, समकालीन भारतीय साहित्य, आजकल आदि तमाम पत्रिकाएं संबंधों और रस्मों को निभाने वाली पत्रिकाओं तक सीमित होकर रह गई हैं।
तो क्या हम सेठाश्रित पत्रिकाओं से उम्मीद कर सकते हैं कि वे उन मूल्यों का भंडाफोड़ करें जिनका समर्थन उनका मालिक करता है। ये बेमानी भी होगा। लेकिन सच तो ये है कि ‘वर्ग संघर्ष’ के स्थान पर अब हमने ‘वर्ग सहयोग’ को अपनाने की आसान व सरल नीति बना ली है। इसके पीछे का दर्शन क्या होता है, इसे भी जान लें...”अरे भाई अब सभी को काटते रहोगे तो कौन बचेगा? अपनी विचारधारा को ऐसे ही लोगों के अंदर रोपना है...शनै शनै।“ उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि अपनी विचारधारा को शनै शनै रोपने का ये दर्शन साहित्य का कितना नुक़सान कर रहा है। या शायद उन्हें मालूम भी हो, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं..क्यों? इसे भी समझना होगा।
सालों पहले एक बार ‘समय माजरा’ पत्रिका में हेतु भारद्वाज ने नाटककार हबीब तनवीर के नाटक ‘जमादारिन’(पोंगा पंडित) पर आपत्ति दर्ज करते हुए दक्षिणपंथी सोच की अपनी टिप्पणी रखी। हेतु भारद्वाज ने इस टिप्पणी में हबीब साहब को एक बड़ा नाटककार तो बताया था, पर उनके काम की नुक्ताचीनी एक सनसनी पैदा करने की गर्ज से की थी। (समय माजरा - अंक 61-62)इस पर मैंने एक लंबी प्रतिक्रिया लिखी, जिसे उन्हांेने इसी पत्रिका के अगले अंक में ज्यों का त्यों छापा मगर एक ‘ग़ैर वाजिब व्याख्या’ होने की टिप्पणी के साथ। (अंक 64) प्रतिक्रियाओं का ये सिलसिला कुछ और अंकों में भी चला। उन्हीं टिप्पणियों एवं प्रतिक्रियाओं के उस दौर में मेरी बात डॉ अजय तिवारी से हुई। ताज्जुब की बात मेरे लिए यह थी कि उसी अंक में अजय तिवारी का भी लेख छपा था जिसमें हेतु भारद्वाज ने हबीब तनवीर पर आक्षेप लगाते हुए चोट की थी, और उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया ज़ाहिर नहीं की थी। ये तबकी बात है जब वे अपने ख़ास कृत्य के लिए कुख्यात नहीं हुए थे और जनवादी लेखक संघ के एक सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर देखे जाते थे। अजय तिवारी का रुख़ चैकाने वाला था - ”तुम इस बाबत अब कुछ ज़्यादा लिखा-पढ़ी न करो, मैं जल्दी ही ‘समय माजरा’ में नियमित काॅलम लिखने जा रहा हूं।“ ‘वर्ग सहयोग’ का यह नमूना मुझे हैरत में रखने के लिए काफ़ी था।
सेठाश्रित एवं बुर्जुआ सोच की पत्रिकाओं द्वारा उस पूरे दौर को छेक दिया जाना समझ आता है जिस दौर में वामपंथी विचारधारा को मज़बूती एवं दिशा मिली। उनके हित कहां जुड़ते हैं - ये भी समझ आता है। ये सब यूं ही नहीं है बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत है। उन सभी कारकों की पड़ताल करना आज के दौर की एक महत ज़रूरत है। विजेंद्रजी की इस पर दो सटीक टिप्पणी देखी जा सकती हैं।
1- ”सेठाश्रित पत्रिकाएं सदैव ही कविता को अग्रगामी विचार रहित तथा चिंतन विमुख बनाने को सक्रिय रही हैं।“
2- बुर्जुआ पत्रिकाओं के संपादक भारतीय मुक्ति संग्राम की अधूरी छूटी क्रांति को अग्रसर करने में लेखकों को प्ररित करेंगे - यह असंभव है।
ये पत्रिकाएं जो पैसे के बल पर अच्छा काग़ज, अच्छी छपाई और अच्छी जिल्द के चलते अच्छे से अच्छे एवं प्रतिबद्ध लेखक को ललचाने के लिए पर्याप्त है। विजेंद्र जी की यह चिंता क़तई वाजिब है कि ”नया लेखक आखि़र प्रकाशन क्यों न चाहे!“ और यहां सवाल नए लेखकों का ही नहीं है बल्कि स्थापित एवं कुछ प्रतिबद्ध लेखकों का भी है जो किसी न किसी बहाने उन पत्रिकाओं को पोषित करते हैं या पोषित होते रहते है। निःसंदेह हमें अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुनः खँगालने की ज़रूरत होती है।
पिछले दिनों विभिन्न राज्य सरकारों ने तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा तमाम हिंदी पत्रिकाओं को सहायता राशि दी जा रही है। इसके चलते बहुत सी मृत प्रायः पत्रिकाएं जि़ंदा होकर पुनः सामने आई हैं। पिछले चार-पांच सालों में पत्रिकाओं की बाढ़ सी आई है। सवाल फिर से वहीं आ कर अटक जाता है कि पत्रिकाएं कितनी व्यावसायिकता के साथ आगे बढ़ें और कितनी साहित्यिक प्रतिबद्धता के साथ इनका तालमेल और संतुलन तय हो? ऐसा भी नहीं हैं कि अच्छी पत्रिकाएं नहीं हैं। कई लघु पत्रिकाएं इससे लाभान्वित होकर अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हैं। कृति ओर, वर्तमान साहित्य, उद्भावना, अलाव आदि कई पत्रिकाएं हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उद्भावना और नया पथ के कई शोधपूर्ण अंक सामने आए हैं। मोटे-मोटे। यह हमेशा बेहतर होता है कि निरंतरता के साथ छोटे-छोटे अंक ही निकलें, पर निकलते रहें, जो पाठकों के अंदर स्वस्थ वैचारिक शृंखला को सतत आगे बढ़ाएं। नया पथ ने इस दिशा में काम को आगे बढ़ाया है। पिछले दिनों विभिन्न प्रतिबद्ध पत्रिकाओं के अंकों में महत्त्वपूर्ण साहित्यकारों एवं कलाकर्मियों की शताब्दी मनाए जाने के उपलक्ष्य में काफ़ी महत्त्वपूर्ण एवं संग्रहणीय सामग्री प्रकाशित हुई है। ये बहुत ज़रूरी है। मगर कई बार मुझे लगता है, इस कारण कहीं वे समसामयिक मुद्दे न छूट जाएं, जिन पर फ़ौरी हस्तक्षेप की मांग होती है। पत्रिका में समसामयिक परिस्थितियों के साथ उनका कितना तालमेल हुआ है और कितना कुछ है जो उसने अपनी विरासत को सँभालने में लगाया है - यह सोचने का विषय है। विरासत में मिले साहित्य के साथ साथ वर्तमान और भविष्य की सामाजिक एवं राजनीतिक चिंताओं पर लगातार बातचीत बेहद ज़रूरी है। जिससे राजनीतिक प्रतिबद्धता एवं दिशा पर बात हो सकती है।
1992 और 2002 की ख़ास घटनाएं - बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना और गुजरात नरसंहार - जब देश की धर्म निरपेक्षता पर सीधे-सीधे न केवल हमला किया गया बल्कि उसके सच को झूठों के तमाम अंबार से ढकने की कोशिश भी की गई, भारतीय लेखकों को ही नहीं, दुनियाभर के लेखकों को उद्वेलित करके गईं।(वी.एस.नायपाल सरीखे बहुत से लेखकों को छोड़ कर जो हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी मौजूद रहे हैं।)। यह हिंदुस्तान के इतिहास में बेहद शर्म की बात रही। अब कोई इन घटनाओं का जि़क्र किए बिना 2012-13 के साहित्यिक रुझानों की बात करे तो यह कहां तक जायज और सटीक होगा। वैसे भी 1992 और 2002 की फ़ासीवादी घटनाओं के बाद की अधिकांश कविताओं में उन कृत्यों का विरोधी स्वर ही अधिक था। उसी प्रकार 70 और 80 के दशक दरअसल देश के निर्माण व उसे एक दिशा (जिसने जन मानस को बेहद प्रभावित किया था।) देने में एक भूमिका निभाकर गए थे। इन दशकों का जि़क्र किए बिना 80 के बाद की कविता पर बातचीत एक तरह से अधूरापन तो है ही, साथ ही इसमें उन आंदोलनों का नकार भी शामिल है जो देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने के साथ-साथ साहित्य में जनवादी धारा का उद्भव एवं विकास के क्रम को दर्शाता है। सवाल ये भी नहीं है कि सिर्फ़ 80 के बाद की कविता या साहित्य का क्या मूल्याकन संभव नहीं है? बिल्कुल है, मगर प्रमुख बात ये है कि उस मूल्यांकन को करने वाले लोगांे की प्रतिबद्धताएं क्या हैं, उनके सरोकार क्या हैं और उनके हित कहां और किसके साथ जुड़ रहे हैं? और इसी चीज़ से उस बात की दिशा और दशा तय होती है।
लोक के सवाल पर विजेंद्र जी अपनी बेबाक टिप्पणी रखते हैं। और लोक के संघर्षधर्मी रूप को सामने लाने की बजाय उत्सवधर्मी रूप को लाने पर चिंता प्रकट करते हैं। लोक के बारे में उनकी समझ न केवल स्पष्ट है बल्कि वे सीधे व साफ़ शब्दों में लोक की अवधारणा एवं उसके महत्त्व को अपने लेखन का हिस्सा भी बनाते हैं। लोक को सिर्फ़ गांव व देहात के साथ जोड़ कर देखने तथा लोक को अमूर्त मानने जैसे अजय तिवारी सरीखे लेखकों के उथले वक्तव्यों पर (जिनमें निःसंदेह छाया प्रतीति की झलक मिलती है सारतत्व की नहीं) विजेंद्र कहते हैं: ”हमें लोक को पुनर्व्याख्यायित कर उसके सही रूप को समझना होगा। लोक को समझकर ही कवि या समीक्षक की लोक दृष्टि बनेगी। मार्क्सवाद में यह लोकदृष्टि व्यापक रूप से अंतर्निहित है क्योंकि वही एकमात्र सर्वहारा का वैज्ञानिक दर्शन है।“ मुझे लगता है हमें विजेंद्र की लोकदृष्टि पर लिखे तमाम साहित्य को पढ़ना व समझना चाहिए। लोक के संघर्षधर्मी रूप को उद्घाटित करते हुए विश्व लोकधर्मी कवियों की श्रंृखला- वाल्ट ह्विटमैंन, लोर्का, नेरुदा, वोल शोयिंका, मायकोवस्की, बाइजुई, नाजिम हिकमत तथा महमूद दरवेश - पर किए जा रहे उनके काम को हमें गंभीरता से पढ़ने की ज़रूरत है।
आखि़र में एक और महत्त्वपूर्ण सवाल है जिस पर मुझे लगता है आज ज़रूर बात होनी चाहिए, जिस पर विजेंद्रजी ने बार-बार लिखा है। वह सवाल है प्रतिबद्धता का। प्रतिबद्धता इंसानियत के प्रति, समाज के प्रति। अब सवाल उठता है कि यह प्रतिबद्धता आती कहां से है? चारित्रिक रूप से पतित व्यक्ति से अच्छे और मानवीय मूल्यों से सराबोर साहित्य की उम्मीद करना बेमानी है। हालांकि वर्तमान स्थितियों में जो हाल है, वह बहुत ही दयनीय है। जिन्हें लोक के बारे में पता नहीं है वही उस पर व्याख्यान देते हुए लोक की अवधारणा तय कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में उस पर अपनी छायाप्रतीति सोच एवं अवधारणा को अपने संबंधों एवं वाक्चातुर्य के चलते लागू करा रहे हैं। और अवसरवादी सोच के शिकार लेखक उन्हें पुष्ट भी कर रहे हैं। चारित्रिक एवं मानसिक रूप से विध्वंसक व्यक्ति से सृजनात्मक साहित्य की उम्मीद करना, साहित्य के प्रति बेईमानी है। आज ये बेईमानी साफ़तौर पर साहित्य में परिलक्षित है। कौन बड़ा लेखक है, कौन छोटा है, किसे चढ़ाना, किसी गिराना है... आदि मनोवृत्तियों के शिकार समीक्षकों की क़तार बहुत बड़ी है जो तमाम अकादमियों पर तो हावी है ही, साथ ही गंभीर साहित्य के क्षेत्र में भी उनका दबदबा बढ़ रहा है। यह एक चिंता का विषय है। क्या आलोचना के इस गिरते स्तर को हमें एक चुनौती के तौर पर नहीं देखना चाहिए? ऐसे में हमारी क्या जि़म्मेदारी बनती है? मुझे लगता है जीवन सिंह, आनंद प्रकाश, अमीर चंद्र वैश्य, रमाकांत शर्मा, रेवतीरमण आदि लोकधर्मी समीक्षकों आदि के साथ-साथ आज हम सबकी जि़म्मेदारी बनती है कि अपनी उसी धार के साथ बुर्जुआ एवं पेशेवर समीक्षकों की साजिश का भंडाफोड़ करें और उनकी असलियत को उजागर करें। अपनी बात को साफ़गोई और बग़ैर किसी लाग-लपेट के कैसे कहा जाता है, इसे हमें विजेंद्र जी से सीखने की ज़रूरत है।
..............................
संपर्क -
17-डी, डी.डी.ए.फ़्लैट्स
मानसरोवर पार्क, शाहदरा
दिल्ली - 110032
फ़ोन - (011)22128079
09312061821
e- mail - ashokkumartiwari@gmail.com

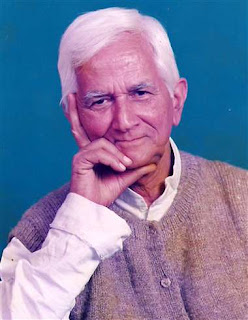


बढ़िया और महत्वपूर्ण आलेख | बधाई
जवाब देंहटाएंसटीक आलोचना ,
जवाब देंहटाएं-नित्यानंद गायेन
बहुत ही सटीक और विचार पूर्ण लेख, कविता और आलोचना के सम्बन्ध पर तीखी टिप्पणी . अशोक भाई को बधाई ...शम्भु यादव
जवाब देंहटाएंइस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.
जवाब देंहटाएंइस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.
जवाब देंहटाएंसमकालीन कविता एवं साहित्य के साथ साथ राजनैतिक हालातों पर एक सटीक टिपण्णी
हटाएंशशी शर्मा
Shaandhaar alekh... lekhak aur bloger dono ka Abhaar.
जवाब देंहटाएंkamchalaun .....
जवाब देंहटाएं