उपासना की कहानी 'कार्तिक का पहला फूल'
 |
| उपासना |
कार्तिक का पहला
फूल
उपासना
कमरे में खामोशी
की सरगोशियाँ थीं। सरगोशियों में सपनों की छटपटाहट थी। सपनों में स्मृतियाँ ही
बचीं थीं अब।
बुढ़ापा उम्र का
रेस्ट हाउस था। ओझा जी को लगता था कि जिंदगी धागे की एक रील है। जिस दिन पूरी उधड़
जाए उसी दिन खत्म हो जाएगी। घड़ी टिक-टिक की रफ्तार से बढ़े जा रही थी। खिड़की से
सूरज का एक नर्म-गर्म टुकड़ा कमरे में बिखरा था। बाहर हल्की हवा के साथ धूल भी थी।
कार्तिक की खुशनुमा सुबह अब दोपहर की तरफ बढ़ रही थी। ओझा जी की हथेलियों की सूजी
नसों में, झुकी-झुकी सी पीठ में, छाती और घुटनों की
पीछे झूलती चमड़ी में जिंदगी ने बाकायदा उम्र की नब्बे दस्तख्तें छोड़ी थीं।
उन्होंने बालिश के नीचे से स्टील की एक नन्हीं डिबिया निकाली।
खैनी धीरे-धीरे
रगड़ कर होठ के पीछे दबा लेने पर वह स्वाद नहीं देती थी, जो स्वाद बायीं हथेली पर रखकर उसे कस-कस कर दूसरी हथेली से
पीटने के बाद अंगूठे से खूब रगड़ कर होठ में दाबने पर आता था। रोज-ब-रोज लगातार
खैनी बनाने के कारण बायीं हथेली के बीचों बीच एक काला मटमैला निशान बन गया था।
खैनी बनाते हुए अक्सरहां ओझा जी खुदरा दिनों की जुगाली करने लगते थे।
जिंदगी खुदरा
दिनों की रोटी कुतरती जाती थी। रोटियाँ इच्छाएं थीं। याद पत्थर थी। सीने पर लदी
रहती थी। ओझा जी ने इन पत्थरों को तोड़-तोड़ कर इन्हें मिट्टी कर दिया था। इस मिट्टी
में ढेर सारे पौधे रोपे गए। दरवाजे पर गुलाबी फूलों से लदी बोगन बेलिया की सघन
बेलें फैली थीं। फिर एक पंक्ति से गुलाब और चमेली के पौधे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर
वृत्ताकार घेरे में गेंदे के पौधे थे। उसके पास ही हरसिंगार और अमरुद के पौधे थे।
एकदम आखिर में उड़हुल का एक पौधा था। यह पौधा वह अपनी नासिक वाली बेटी के यहाँ से
लाये थे। पौधे फकत फूल-फल के ही नहीं थे। कुछ जंगली पौधों की पत्तियाँ व डालें इस
खूबसूरती से छाँटी गयी थीं कि उनसे उस नन्हे से आंगन की खूबसूरती कई गुना बढ़ गयी
थी। यह सब कोई नई बात नहीं थी।
पारसनाथ में रेलवे
के ओपन लाइन में जब ओझा जी थे तब भी उनके क्वार्टर का दो बित्ता भर बागीचा खूबसूरत
फूल-पौधों से सजा रहता था। एक बार तो जी० एम० ने उन्हें सौ रुपये का ईनाम भी दिया
था। ओझा जी को अपने पौधों पर बहुत गर्व था। उन पर ठहरने वाली एक प्रशंसात्मक
दृष्टि ओझा जी का रोआँ-रोआँ पुलकित कर देती थी।
खैनी खा कर वो
उठे। जनेऊ को आहिस्ता-आहिस्ता पीठ पर रगड़ते हुए आँगन में आये। एक-एक पौधे के पास ठहरे।
रात भर झरे सूखे हरसिंगार और भूरी पत्तियाँ उन्होंने सुबह ही चुन कर साफ कर दी थी।
मिट्टी में पर्याप्त नमी थी। उड़हुल के अलावा अन्य किसी पौधे पर फूल या कली नहीं आई
थी। जिस तन्मयता से चित्रकार कैनवास पर रंग भरता होगा...जिस ममता से माँ अपने शिशु
को दूध पिलाती है,
ओझा जी उसी
मोह-ममता-तल्लीनता से मिट्टी की निराई-गुड़ाई करते। पौधों में पानी देते। धोती उनकी
मिट्टी से लिसड़ जाती। नाखूनों में जमी मिट्टी टीसने लगती थी। पर पौधों से मोह बढ़ता
ही जा रहा था। एक-एक पत्ता, बूटा-बूटा उनकी
छुअन जैसे पहचानता था।
माँ का सबसे कमजोर
बच्चा माँ की सबसे ज्यादा ममता पाता है। उड़हुल का यह पौधा ओझा जी का ऐसी ही कमजोर
संतान था। अब तक कभी इसपर एक भी फूल नहीं पनपा था। पत्ते चिकने-चमकीले-सुन्दर थे।
टहनियां भी सुडौल थीं। ओझा जी भी अक्सर पौधे की छँटाई करते। समय से खाद-पानी सब
होती। उसकी चिकनी पत्तियों को प्रेम से सहलाते। उनकी नसों में बहता हुआ स्नेह और
जीवन जैसे कतरा-कतरा पौधे तक संप्रेषित होता रहता। उसे मिनटों निहारते। और...दो
दिन पहले ही ओझा जी ने उसपर गुनगुनाती हुई नन्हीं कली देखी थी। कली अब-तब खिलने की
स्थिति में है। ओझा जी ने आहिस्ता से कली को छुआ। मुस्कुराये। पनोहा पर आ गए।
नहाने के लिए चापाकल चलाते वक्त पैर की नसें तड़-तड़ करती थीं। पूरी देह टटाती थी।
बूढ़ा आदमी देह से नहीं हिम्मत से चलता है। हिम्मत ही थी वह, जो मानने ही नहीं देती थी कि अब उनकी देह थक रही है। यद्यपि
वे स्वयं सबसे कहते,
-‘बड़ी उमिर हो गइल
बा हमार!’
पर यही हिम्मत तब
चुकने लगती जब बुखार सिर पर चढ़ने लगता। या पेट परेशान करने पर उतारू हो जाता। ओझा
जी अक्सर ही कहते,
-‘प्राण को देह से
बहुत मोह होता है। प्राण जल्दी देह नहीं छोड़ना चाहता। पर देह तो अयोग्य हो जाती
है। इसी मोह के कारण मृत्यु के समय आदमी को कष्ट होता है।'
जब-तब यही मोह उन्हें बाँधने लगता। छूटी हुई चीजों और लोगों का मोह...मित्र, परिजन, बंधु, पत्नी। और पौधों का मोह तो था ही। इस मोह का कोई अर्थ है क्या? छूटी हुई चीजें और लोग पास नहीं थे। और जो नहीं छूटे थे। वो भी आखिर कितने घड़ी पास हैं इसका कोई ठिकाना है?
जब-तब यही मोह उन्हें बाँधने लगता। छूटी हुई चीजों और लोगों का मोह...मित्र, परिजन, बंधु, पत्नी। और पौधों का मोह तो था ही। इस मोह का कोई अर्थ है क्या? छूटी हुई चीजें और लोग पास नहीं थे। और जो नहीं छूटे थे। वो भी आखिर कितने घड़ी पास हैं इसका कोई ठिकाना है?
‘नमामीश मिशान निर्वाणरूपं...’
कपाट अरसा हुआ
छूटे। छोटा सा शिवलिंग कोने में धकेल दिया गया था। उन पर अब बेलपत्र नहीं चढ़ता।
कमरे में काठ का एक काला बक्सा था। बक्से में ढेर सारी पुरानी किताबें और
पत्रिकाएँ थीं। बानवे-तिरानवे तक की कादम्बिनी के अंक थे। कभी बहुत चाव से
उन्होंने ये किताबें खरीदी थीं। उनपर दुलार से अखबार की जिल्द मढ़ी थी। अब तो इस
तरफ देखने तक का मन नहीं करता। बक्से में धूल अंटा पड़ा था। ओझा जी कपड़े से धूल झाड़
कर किताबें सजा रहे थे। बहू खाना लेकर आई थी,
-‘बाबूजी खाना।‘
-‘रख दो।‘
ओझा जी पूर्ववत
किताबें सजाते रहे। बहू खाना-पानी रख कर चली गयी। किताबें रखकर उन्होंने बक्सा बंद
कर दिया। सामने खाने की थाली थी। खाना देखकर उन्हें पत्नी बेतरह याद आती थी। पत्नी
को तब नाम से पुकारे जाने का चलन नहीं था।
-‘सुन तारु हो...!’ ही कह कर काम चला लिया जाता था। पत्नी खामोशी से ही आगे-पीछे डोलती रहती थी।
उनके आसन पर बैठ जाने के बाद ही थाली में गरम खाना परोसती। ओझा जी जितनी देर खाते
वो बेना डोलाती रहती थीं। उन्हें सब्जी तीखी चाहिए होती तो तीखी ही मिलती। मीठा
खाने का मन होता तो मीठा हाजिर हो जाता था। ओझा जी काम में भिड़े रहते। पत्नी
बार-बार पहले खाना खा लेने की चिरौरी करतीं। वह सुनी-अनसुनी कर देते। काफी वक्त
बाद मनमौजी काम निपटा कर आते। बावजूद इसके खाना गर्म ही मिलता।
उस दिन बारिश हो
रही थी। बागीचे के हर पौधे तक पानी जाने के लिए वो करहा तैयार कर रहे थे कि पत्नी
पकौड़ियाँ लेकर बरामदे में हाजिर। पत्नी बार-बार पहले गर्म पकौड़ियाँ खा लेने का
आग्रह कर रही थीं। उन्होंने बुरी तरह झिड़क दिया था,
-“हर समय क्या ‘खा लीजिए’...’खा लीजिये’ लगाये
रखती हो। देखती नहीं काम निपटा रहा हूँ। तुम्हें तो बस अपने पकौड़ियों की पड़ी है।“
पत्नी शायद अन्दर
तक आहत हो गयी थीं। धीरे से बोलीं थीं,
-‘जब हम ना रहब न तब
बुझाई तहरा...’
दोपहर किसी उदास
पुराने धुन की तरह चढ़ रही थी। खाने पर मक्खी भिनभिनाने लगी। ओझा जी ने हथेली हिला कर
मक्खी भगा दी। दीवार के कोनों पर मकड़ी के जाले लटक आये थे। खिड़की पर बैठा कबूतर
पंख फड़फड़ाता उड़ गया।
सुबह-सुबह उठ कर
ओझा जी पौधों को सुप्रभात कहने आये तो उड़हुल पर एक नन्हा फूल खिल चुका था। उजले
फूल की पंखुड़ियों के निचले सिरों पर कत्थई रंग के धब्बे थे। पूरे बागीचे में मौसम
का पहला फूल शर्माया-शर्माया सा मुस्कुरा रहा था। अरहर की झाड़ से आंगन बुहारते हुए
कई दफे नजर उधर ही को उठ जाती। जैसे कत्थई स्याही में ऊँगली बोर कर उजले फूल पर
छिड़क दिया हो। जिसकी भी थी बड़ी खूबसूरत कलाकारी थी यह। दिन फूल के इर्द-गिर्द, उससे ही सराबोर गुजरा। कार्तिक की संतरई शाम अब भागने लगी
थी। हवा से दूब झूम रहे थे। एक पोता ओझा जी के पास ही बैठा मोबाईल चला रहा था।
बच्चों को मोबाईल चलाते देख कर ओझा जी को जैसे कुछ होने लगता था। कोई उलझन या ऐसा
ही कुछ।
-‘का टीप-टाप कर रहे
हो?’
-‘कुछ नहीं’। पोते
ने व्यस्त भाव से कहा।
किसी का भी अपने
पास बैठना कभी-कभी ओझा जी को रोमांच से भर देता था। बीते दिनों की मौखिक जुगाली
करने के लिए मन कुलबुलाने लगता। पर अब स्मृतियाँ, वर्त्तमान सोच, कल्पनाएँ, स्वप्न सब इस कदर गड्ड-मड्ड हो गए थे कि एक-एक सूत को
अलगाना अब मुश्किल लगता था। कुछ भी कहने से पहले मन ही मन जैसे कोई तैयारी चलती थी।
सोचे हुए और बोले हुए का फर्क मिट गया-सा लगता था। कई बार कुछ बातें ओझा जी मन में
इतना दुहरा लेते कि उन्हें ऐसा लगता कि वो इसे दूसरों को कई दफे सुना चुके हैं। कई
बार इसके उल्टा भी होता था कि दूसरों से कई बार कही हुई बातें भी मन में दुहराई
गयी-सी लगती थीं। दिन भर कमरे में ओझा जी की सांस के अलावे बस चूहों की भागदौड़
सुनाई पड़ती थी। ऐसे में बोलती हुई टी० वी० भी निर्जीव नहीं लगती। ओझा जी ने खंखार कर
कुछ पंक्तियाँ कहना शुरू किया था। पोते ने ऊबे व विरक्त भाव से कहा
-‘सुनाई हुई कहानी
कितनी बार सुनायेंगे बाबा?’
ओझा जी के पास आगे
कहने के लिए कुछ नहीं बचता था।
दुनिया के हर आदमी
के पास एक त्रिभुज था। तीखे कोणों वाला त्रिभुज। ओझा जी के भीतर भी कोई त्रिभुज
था। ओझा जी अपने भीतर के त्रिभुज को लगातार घिसते रहते थे, कि वह कोमल, नर्म एवं गोल बने
रहे। ताकि जब भी किसी से उनका त्रिभुज टकराए तो सामने वाले को कम से कम चोट
पहुंचे। लेकिन दुनिया के पास न तो इतना धैर्य होता था न वक्त...इसलिए ओझा जी से
टकराने वाले दुनिया के हर त्रिभुज की चोट बेहद मारक होती थी। यादों की रेत जब जी
चाहे जिधर फिसल जाती थी। पाँच बेटियों में जब सबसे बड़ी सायानी हुई तो ओझा जी ने
मँझले भाई से वर ढूँढने में मदद मांगी। भाई साँझ की बाती में घी डालते हुए बोले थे।,
-‘सेठ टोडरमल कहता
है कि भाई बेटी अपने दम पर पोसता है कि भाई के दम पर।‘
ओझा जी चुप।
धीरे-धीरे सारी बेटियाँ अपने-अपने घर की हो गयी थीं। छुट्टियों में उनसे मिलने
आतीं। दुलार जताया जाता। शिकायतें दर्ज होतीं,
-‘आप छोटी को ज्यादा
मानते हैं।‘
-‘आप बड़ी को ज्यादा
मानते हैं।‘
शब्द की कई तहें
थीं। एक शब्द से कई अर्थ साधे जा सकते थे। ओझा जी मानने से थक गए थे।
हवा में खुनक बढ़
रही थी। सूती शाल बदन पर ढीली पड़ गयी थी। अँधेरा गाढ़ा था। ओझा जी लालटेन जलाने
कमरे में जाने लगे। आंगन के कोने में उड़हुल मुस्कुरा रहा था। ओझा जी उसके पास गए।
उसकी पंखुड़ियों का मोती-सा उजलापन चमक रहा था। ओझा जी धीमे से फुसफुसाए,
-‘तुम्हारे पास तो
कोई त्रिभुज ही नहीं है?’
कार्तिक के एक
हल्के झोंके से फूल सिहर गया।
सुबह ओझा जी सबसे
पहले हरसिंगार के पास गये। उसके फूल चुन कर ओझा जी फेंकते नहीं थे। उन्होंने सारे
फूल पेड़ की जड़ों के चारों ओर गोल घेरे में रख दिये। क्यारियों की ईटें टेढ़ी-मेढ़ी
हो गयी थीं। ईटें सीधी करती हुई ओझा जी की नजर अनायास ही उड़हुल पर गयी थी। डाल
सूनी थी। ओझा जी का दिल धक से हो गया। किसने किया यह? उन्होंने बहू को आवाज लगायी...
-‘यह उड़हुल का फूल
किसने तोड़ा?’
-‘आज एकादशी है तो
पूजा के लिए मैंने ही तोड़ लिया।‘ बहू धीरे से बोली।
ओझा जी का मन
रोने-रोने को हो आया। वह चुपचाप बैठकर क्यारी की ईटें सही करने लगे। बोगन बेलिया
की लताओं के पास छत पर कबूतर था। कबूतर टुकुर-टुकुर ओझा जी को देख रहा था। उड़हुल
की वह सूनी डाल कार्तिक के झोंके से अब भी झूम रही थी।
सम्पर्क
ई.मेल - chaubeyupasana@gmail.com
(इस पोस्ट में प्रयुक्त पेंटिंग वरिष्ठ कवि विजेन्द्र जी की है.)
(इस पोस्ट में प्रयुक्त पेंटिंग वरिष्ठ कवि विजेन्द्र जी की है.)

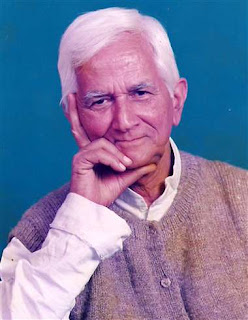


Itni sundar rachna....kaise..observe..kar leti hain
जवाब देंहटाएंaap..upasnaji...adbhut
Himanshu mishra
Itni sundar rachna....kaise..observe..kar leti hain
जवाब देंहटाएंaap..upasnaji...adbhut
Himanshu mishra