सर्वेश सिंह की कविताएँ
 |
| सर्वेश सिंह |
समय का मापन करने वाले भले ही उसे भूत, भविष्य और वर्तमान के खांचे में बांटे, कवि तो उसे अपनी संवेदनाओं में ही मापता है. इस संवेदना में संभावनाओं के लिए भरपूर जगहें हैं जिसे कवि बचाए-बनाए रखना चाहता है. सर्वेश सिंह ऐसे ही युवा कवि हैं जो विद्रूपताओं भरे इस समय में संभावनाओं को बचाए रखना चाहते हैं. इस क्रम में वे 'पीछे जाना' जैसी कविता लिखने का साहस भी दिखाते हैं. आज लगातार आगे बढ़ने की जो अंधी दौड़ चल रही है उसमें यह साहस दिखाना काबिले तारीफ़ है. यह 'पीछे जाना' उस मनुष्यता को बचाए रखने के लिए पीछे जाना है जो आगे जाने की होड़ में कहीं गायब सा हो गया है. ऐसी ही भावनाओं वाले कवि सर्वेश सिंह की कविताएँ हम पहली बार के पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं.
जन्म- 25 जून, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
जन्म- 25 जून, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
शिक्षा : एम.ए.,एम.फिल.,पी-एच. डी.,
जे.एन.यू., दिल्ली से
सर्वेश ने कहानी, कविता, आलोचना जैसी विधाओं में काम किया है.
हंस, आलोचना, आजकल, उम्मीद जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं सहित करीब तीस पत्रिकाओं में आलेखों का प्रकाशन. पाखी, परिकथा और जनसत्ता में कहानियाँ प्रकाशित. आउटलुक और परिकथा में कविताएँ प्रकाशित.
हंस, आलोचना, आजकल, उम्मीद जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं सहित करीब तीस पत्रिकाओं में आलेखों का प्रकाशन. पाखी, परिकथा और जनसत्ता में कहानियाँ प्रकाशित. आउटलुक और परिकथा में कविताएँ प्रकाशित.
आलोचना की एक पुस्तक: 'निर्मल वर्मा की कथा-भाषा’ प्रकाशित
सर्वेश सिंह की कविताएँ
एकोहम बहुस्यामि.....
बटुक ने उसे पंचामृत में डुबोया
और आरण्यकों में प्रक्षिप्त कर दिया
पुजारी ने लपेटा गेरुवे में
और आरती की थाल में सजा दिया
एक बूढ़े समीक्षक ने परखा बहुरंगी चश्मों से
और इतिहास के ऊपर उछाल दिया
जब हाथ आई एक चौड़े जननायक के
तो उसने नारे में बदल दिया
छात्रों ने उसके कतरों में पाए सन्दर्भ
पढ़ कर ठहर गया बंझा को गर्भ
ब्राह्मण ने लगाई पुराणों की दौड़
क्षत्रिय का अश्व लेकर भागा चित्तौड़
बनिए की तिजोरी की चोर बन गई
शुद्र की थाली का कौर बन गयी
देवताओं की अमृत बनी
असुरों की विष
शाला की मन्त्र बनी
वामा की तंत्र
बुद्ध की दुःख हुई
गौतम की न्याय
कबीर का क्रोध बनी
तुलसी की सहाय
कोई मक्का लेकर भागा
कोई काशी
कहीं कठौते की गंगा बनी
कहीं सत्त्यानाशी
बिस्तर पर कामसूत्र बनी
कुरुक्षेत्र की गीता
किसी ने केवल राम देखा
किसी ने सीता
रूस हुई फ़्रांस हुई
हुई भगवा और वाम
कभी केवल रूप हुई
कभी केवल नाम
कविता तो एक थी
बस सुविधा की व्याख्याओं से
बहुस्यामि हो गई........
मन्त्र-फाट
वहाँ जूते उतार कर जाते हैं
जैसे बिस्तरों पर
द्वार पर नंदी है-
उत्तुंग और उत्तेजक
अंगूठे और तर्जनी की योग-मुद्रा से उसे आभार दें
यहाँ से अब वापसी मुश्किल है
ध्यानावस्थित मन
लसलसे रास्तों पर
खुद-ब-खुद आगे बढ़ता जाएगा
खून में मुक्ति की चाहना के काबुली घुड़सवार
दौडेगें सरपट
एक-सा ही जादू है
यहाँ भी..
और वहाँ भी..
कि मन की अज्ञानता में
गर्भ-गृह के द्वंद्व की सुखद यातना में
एक गति, एक ताल और एकतानता में
सारी ये कायनात
मंथनमय है
और वहां जहाँ गिरता दूध जमा हो रहा है
और गल रहे हैं फूल, बेल-पत्र
वह आकृति, रूप के भवन में दीप की शिखा-सी है
त्रिभंगी और लसलसी
वह बिस्तरों की सत्यापित प्रतिलिपि-सी है
देवताओं में सुडौल वे
सनातन काल से वहीं जमे हैं
पत्थर के चाम हो गए हैं
पर पत्थरों के इस विन्यास में
कितना तो साफ़ है
धर्म का उद्योग
कितना तो उज्ज्वल है उनका
चिर-संयोग
कितना तो समान है
कि बिस्तरों में उस कामना के बाद
जागना नहीं
और जागरण इस प्रार्थना के बाद भी नहीं
कर्म के बस दो अलग-अलग तन्त्र हैं
आस्था और वासना
श्रेयस और प्रेयस
फट कर अलग हुए
पर एक ही मन्त्र हैं
कर्म के बस दो अलग-अलग तन्त्र हैं
आस्था और वासना
श्रेयस और प्रेयस
फट कर अलग हुए
पर एक ही मन्त्र हैं
वही है पर देता नहीं दिखाई!
खून के आख्यान
उसी की सर्जना हैं
वही कहानी में किस्से को रुलाता है
और गद्य की क्रियाओं के हाथों में धरता है आग
भड़काने को साहित्त्य के इतिहासों में
उसी का शब्द-कौशल है कि
जीवनी के मुंह पर है कालिख
और आत्मकथा का कलेजा है दो फाट
उसे देख सकते हैं आप
निबंध के उन्नत पहाड़ों पर
कुटज की जड़ों में मट्ठा डालते हुए
और संस्मरण के हर दूसरे वाक्य की छाती पर
पैर हिलाते रचनारत है जहाँ वह यमराज की तरह
लोग नहीं मानते पर
आलोचना की ध्वनियों तक से
जुड़े हैं उसके गुप्त तार
और अब तो हर दर्शक जानता है कि
बेचारे नाटक को रंगमंच तक
पकड़ ले जाते हैं उसके ही सवार
बेचारी लघुकथा तो है अब उसकी सैरगाह भर
और कविता है आरामदेह बिस्तर
नहीं होता विश्वास तो निकलिए कल्पना से बाहर
और देखिए जमीन पर
कि कैसे
वह पद्य में देता है भाषण
और गद्य में करता है शासन
इतना बारीक फ़रक
भला कहाँ होगा
किसी और लेखक में
इसीलिए
अगर व्यंजना में देखें
तो कहना न होगा
कि जैसे घेरे है कण-कण को ब्रह्म
साहित्य को ठीक वैसे ही
घेरे
वही है पर देता नहीं दिखाई
सड़क पर आँख
सड़क पर
वह अचानक खुल जाती
है
अदब से बाएं चल कर देखें
चौराहे फैलते हैं
हवा के हरे पत्ते
रबड़ के बिस्तर हैं
धूप पेड़ की ओट से
देखती है छाया का तांडव
ध्वनियों पर बढ़ रहा
आसमानी दबाव
बाजार का मुँह बनता है
चेहरे के कन्धों पर
कविता का जनाजा निकलता है
लौटना साहित्य नहीं
और बदलना है
भाव
भाग कर देखो वहाँ जहाँ यथार्थ हो
मोड़ से सड़क दोगली
हो जाती है
पूरब को
गद्य-पथ
और पद्य-पथ पश्चिम
को
रचने को मुड़ें
कि
इस पार के नाटक की
आँधियां
उस पार की कथाओं के
तूफानों में फेंकती हैं
उपन्यासों का कितना
तो मैला आँचल!
मछेरी आलोचनायें
निकालती हैं दलदल से
और खड़ा कर देती हैं
सड़क के बीचों बीच
जहाँ आत्मकथाएं
रोती हैं
ध्यानमग्न निबंधों
की गहनता
जिन्हें करुणा से देखती
हैं
देखने से ज्यादे
आँखों के लिए कितना
कुछ और है
रचने को
सड़क के दिक्-काल
में
पीछे जाना
पीछे ही जाना हो
तो जाना नहीं समा
जाना
और उधर से जाना
जिधर से सूरज
निकलता है
कोई चश्मा पहन कर भी मत जाना
नहीं तो समा नहीं
पाओगे
बच्चो-सी आँखें ले
जाना
तब तुम इतिहास नहीं
कुछ और देखोगे
आंसूओं के चहबच्चे
पैरों से लिपट
सुनाएगें तुम्हें
अपनी राम कहानी
और ऊपर पत्थर की
खिडकियों से झांकती
सत्तर की सूनी
आँखें
दिखायेंगी तुम्हे
मनुष्य का असली अतीत
स्मृति में तुम्हारे
साजिशें भरती गयी हैं
इसीलिए फिर कह रहा
हूँ
कि चश्मा पहन कर
और डूबते सूरज की
तरफ से
मत जाकर समाना
कुछ नहीं पाओगे
तुम आज अचंभित हो
कि तुम्हारे प्रेम
में कोई स्वाद नहीं है
और मैं कहता हूँ कि
इसका कारण है
बहुत पहले की एक
स्त्री के सर्पीले बाल
जो भरी सभा में
सपना देख रहे हैं
किसी के खून से
धुलने का
और शायद उससे भी
पहले की एक स्त्री की करूण प्रार्थना
कि ये धरती फट जाए
और मैं रहूँ उसके
गर्भ में
इस धनुष-बाण की
संस्कृति से बाहर
आँखों को उँगलियाँ
बना टटोलना
वचनों से
टुकड़े-टुकड़े हुआ प्रेम
वहीं कहीं लथपथ पड़ा
होगा
एक बात और याद रखना
पुष्पक से मत जाना
दबे पांव जाना
झोले में कविता
कविताएँ रख ली हैं मैंने
झोले में
और निकल पड़ा हूँ अतृप्त
इच्छाओं की काल यात्रा पर
घर से निकलते ही
उनमें से कुछ ने
जोड़ लिए हैं हाथ
और हो गयीं हैं
ध्यानमग्न
कि जैसे टूटने ही
वाली हो धर्म की कोई मरजाद
और कुछ हो गयीं हैं
गहरे उदास
कि जैसे अनैतिक बता कर फाड़ दिया जाने वाला हो कोई प्रेम-पत्र
कंधे में उनकी संभावनाएं महसूस करते
खोज रहा हूँ समय का
वह हिस्सा
जो फिलहाल न भूत
में
न भविष्य में
और न ही वर्तमान
में है
कि शायद किसी
अन्तराल में मिले
वह गहरे कानों वाली
खूबसूरत स्त्री
जिसे सौंप कर इन्हें
जिसे सौंप कर इन्हें
यह देखूँ
कि जब एक कवि
और उसकी कविताएँ
और एक ख़ूबसूरत
स्त्री
मिलते हैं
तो वहाँ बना रहता
है अँधेरा
या लपेटता है उसे प्रकाश
संपर्क:
अध्यक्ष, हिंदी विभाग,
डी.ए.वी.पी.जी.कॉलेज, (बी.एच.यू.)
औसानगंज,वाराणसी- 221001
मो.- 09415435154
Email: sarveshsingh75@gmail.com (इस पोस्ट में प्रयुक्त पेंटिंग्स वरिष्ठ कवि विजेन्द्र जी की हैं.)



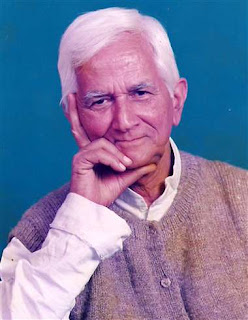


bahut achhi kavitayen
जवाब देंहटाएंइन कविताओं का शिल्प अपने आप में अनोखा है। और यह भी सबसे महत्व की चीज है कि संवेदना के जिस स्तर पर ये कवितायें गंभीर हैं वहाँ सोंचने और समझने के बाबत ठहरने की काफी गुंजाइश बनती है । बड़े भाई सर्वेश सिंह जी को बधाई इन शुभकामनाओं के साथ कि वह मनुष्यता के पथ पर कविताई के साथ मुखर रहें और संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो "पहली बार" जैसे महत्वपूर्ण ब्लॉग को बराबर लगातार रचनात्मक ऊर्जा देते रहते है बिना नागा किए !
जवाब देंहटाएं