गिरीश चन्द्र पाण्डेय ‘प्रतीक’ की कविताएँ
 |
| गिरीश चन्द्र पाण्डेय ‘प्रतीक’ |
परिचय-
डॉ
गिरीश चन्द्र पाण्डेय "प्रतीक"
शिक्षक
उत्तराखंड शिक्षा विभाग
सम्प्रति
- पिथौरागढ़ जनपद में कार्यरत
साहित्यिक यात्रा-
एक
काव्य संग्रह "आइना" प्रकाशित, इंद्रधनुष, पहाड़ का दर्द, कविताओं के रंग आदि संयुक्त काव्य संग्रहों
में स्थान मिला है। राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित, आकाशवाणी से कविता-पाठ आदि
कवि
का अपनी कविता के बारे में वक्तव्य :
कविता
लिखना आसान हो सकता है। पर कविता को जीना उतना ही
मुश्किल। असली कविता वही है जिसे हम खुद में जी रहे हों। समाज को एक नयी दिशा
देने का दम कविता में होना चाहिए। सामाजिक सरोकार अगर कविता में नहीं होंगे
तो कविता में भटकाव निश्चित है। जिसे समाजोपयोगी, लोकहितकर नहीं कहा जा
सकता।
हम जब से आज़ाद हुए हैं 'विकास' शब्द सुनने के अभ्यस्त हो गए
हैं। 68 वर्ष बीतने के बावजूद विकास शब्द
जहाँ का तहाँ है। आज के भारत के 70 % से अधिक लोगों की आय एक डालर से कम
है। बेरोजगारी, बदहाली, गरीबी, भूखमरी, अकाल आज भी देश के लिए बड़ी समस्याएँ
बनी हुई हैं। ऐसा नहीं कि विकास के मद में कम पैसा खर्च हो रहा हो। फिर वजह
क्या है कि समस्याएँ और विकराल ही हुई हैं। आज भी राजनीतिक दल जाति, धर्म, सम्प्रदाय, बोली, भाषा, क्षेत्रीयता आदि के मुद्दों को उठा कर लोगों को
आपस में उलझा कर अपना हित साधते रहते हैं। राजनीति में कदम रखने वाला
व्यक्ति और उसका परिवार चंद दिनों में ही पूंजीपतियों की बराबरी करने
लगता है। ऐसे में राजनीति जिसका साधन बन गयी है वह प्रत्यक्ष है। कवि गिरीश चन्द्र पाण्डेय
प्रतीक 'विकास' के इस रहस्य को अपनी कविता में उद्घाटित
करने का साहस दिखाते हुए कहते हैं - 'विकास हुआ है/ कुछ चंद विकसित
लोगों का/ मैं ये भी नहीं कह रहा विकास
नहीं हो रहा है/ हो रहा है/ पर विकास कम विनाश ज्यादा/ असन्तुलित
भौतिक विकास/ नहीं हुआ हमारी नैतिकता./ और
हमारे विचारों का विकास/ हम ज्यादा संकीर्ण हुए हैं/ पहले से अब'। यह
सुखद है कि गिरीश क्षेत्रीय शब्दों से समृद्ध हैं। उनके पास इन्हें कविता में
बरतने का हुनर है। इसकी बानगी यहाँ प्रस्तुत कविताओं में स्पष्ट तौर पर दिखाई
पड़ेगी। तो आइए आज पढ़ते हैं गिरीश चन्द्र पाण्डेय प्रतीक की कविताएँ। इन कविताओं को
हमें उपलब्ध कराया है चर्चित कवि महेश चन्द्र पुनेठा ने।
गिरीश चन्द्र पाण्डेय ‘प्रतीक’ की कविताएँ
अब की बार
इससे बड़ी निराशा और क्या होगी
जब खेत में पड़ा पोसा
देखा रह जाय
बोने को रखा गया बीज
चक्की के हवाले हो जाए
कारी गयी हलानी
छिले गए सूले
न्या पाते
हो जाएँ चूल्हे के हवाले
पूष की रात
आग तापने के बाद
पेट की आग
जो बुझ रही है
गरीबी रेखा के
गेहूं चावल से
दाल जो चिढ़ा रही थी मुँह
जेब के आर पार कुछ तो न था
दिन भर जेब ही तो टटोली थी
काम क्या करता
एक पैग शराब
जो पिलाई थी हौलदार ने
मोड़ से सामान लाने के एवज में
बढ़ गया था परिवार
एक अदद पूत के लिए
चार कन्याओं के बाद
कुल जमा सात
जिनको जिन्दा रहना था खेत के सहारे
और गोठ में बँधी कामधेनु
जो बैली थी
पिछले चौमास से
पराल खा राल टपका रहा था बैल
लाल पड़ गए थे खुर
जाये तो जाए कहाँ
चरने की जगह
उग आयी थी
सिमरी
बादल आया था शाम को
हवा के झोके को सह न सका
और उड़ गया
परिंदे के मानिंद
एक आशा जो जगी थी
वो फिर ........
जब खेत में पड़ा पोसा
देखा रह जाय
बोने को रखा गया बीज
चक्की के हवाले हो जाए
कारी गयी हलानी
छिले गए सूले
न्या पाते
हो जाएँ चूल्हे के हवाले
पूष की रात
आग तापने के बाद
पेट की आग
जो बुझ रही है
गरीबी रेखा के
गेहूं चावल से
दाल जो चिढ़ा रही थी मुँह
जेब के आर पार कुछ तो न था
दिन भर जेब ही तो टटोली थी
काम क्या करता
एक पैग शराब
जो पिलाई थी हौलदार ने
मोड़ से सामान लाने के एवज में
बढ़ गया था परिवार
एक अदद पूत के लिए
चार कन्याओं के बाद
कुल जमा सात
जिनको जिन्दा रहना था खेत के सहारे
और गोठ में बँधी कामधेनु
जो बैली थी
पिछले चौमास से
पराल खा राल टपका रहा था बैल
लाल पड़ गए थे खुर
जाये तो जाए कहाँ
चरने की जगह
उग आयी थी
सिमरी
बादल आया था शाम को
हवा के झोके को सह न सका
और उड़ गया
परिंदे के मानिंद
एक आशा जो जगी थी
वो फिर ........
**बाटुली**
बहुत ठण्ड थी
भजालि में रख दिए थे गौत
आग भुरभुरा रही थी
आमा तुरंत याद करती
अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को
उन्हें क्या लेना-देना
विज्ञान के नियम से
बेटे का नाम लेना
आग का भुरभुरना
बंद होना
और आंसुओं का झरना
लकड़ियों को ठेशना
और यादों का पल में गुजर जाना
उन यादों से लिपटे
सेकवा गँदरेना की महक
तौली में गुड़गुडाता अध्यानी का पानी
चावल पड़ते ही
जो हो गया था मौन
पर आमा तो मचल रही थी
उस गिलास
उस थाली को देख कर जो अब छोटी हो गयी थी
बेटे के लिए
पक गयी थी गौतानि
आमा ने पस्का था
सबके लिए
इतने में शुरू हुई
बाटुली की झड़ी
फिर याद आया वही बेटा
वही यादें
वही आंशु
क्या लेना देना था आमा को विज्ञान से
नाम लेते ही रुक गयी थी बाटुली
नाती बोला आमा
क्या पापा को भी
बाटुली लगी होगी
आमा......
निश्शब्द...........
भजालि में रख दिए थे गौत
आग भुरभुरा रही थी
आमा तुरंत याद करती
अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे को
उन्हें क्या लेना-देना
विज्ञान के नियम से
बेटे का नाम लेना
आग का भुरभुरना
बंद होना
और आंसुओं का झरना
लकड़ियों को ठेशना
और यादों का पल में गुजर जाना
उन यादों से लिपटे
सेकवा गँदरेना की महक
तौली में गुड़गुडाता अध्यानी का पानी
चावल पड़ते ही
जो हो गया था मौन
पर आमा तो मचल रही थी
उस गिलास
उस थाली को देख कर जो अब छोटी हो गयी थी
बेटे के लिए
पक गयी थी गौतानि
आमा ने पस्का था
सबके लिए
इतने में शुरू हुई
बाटुली की झड़ी
फिर याद आया वही बेटा
वही यादें
वही आंशु
क्या लेना देना था आमा को विज्ञान से
नाम लेते ही रुक गयी थी बाटुली
नाती बोला आमा
क्या पापा को भी
बाटुली लगी होगी
आमा......
निश्शब्द...........
गौतानि = गहत एक दाल द्वारा निर्मित एक विशेष
पहाड़ी दाल का रूप जो पकाने के बाद उसके दाने अलग और शूप अलग लोहे की कढ़ाई में धीमी
आंच में पकता है
भजालि = लोहे को भारी और गहरी कढ़ाई
पस्कना = खाना परोशना
बाटुली = हिचकी
गन्द्रेना = पहाड़ी जड़ी जिसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है
शेकवा =यह भी एक मसाला ये दोनों उच्च हिमालयी क्षेत्र में पायी जाती हैं
तौली=ताम्बे या पीतल से बना बंद गले का गागर नुमा भांड
अध्यनि=चावल डालने से पहले गरम करा गया चूल्हे में रखा गया उबलता पानी
भजालि = लोहे को भारी और गहरी कढ़ाई
पस्कना = खाना परोशना
बाटुली = हिचकी
गन्द्रेना = पहाड़ी जड़ी जिसे मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है
शेकवा =यह भी एक मसाला ये दोनों उच्च हिमालयी क्षेत्र में पायी जाती हैं
तौली=ताम्बे या पीतल से बना बंद गले का गागर नुमा भांड
अध्यनि=चावल डालने से पहले गरम करा गया चूल्हे में रखा गया उबलता पानी
नदी
नदी किनारे का गाँव
जामुन की छाँव
न पानी ही नसीब
न जामुन ही करीब
जामुन की छाँव
न पानी ही नसीब
न जामुन ही करीब
एक फौंला पानी
जेठ की झूर दोपहरी में
भरने गयी थी नानी
नंगे पाँव
गङ्गलोडों से चढ़ते उतरते
अपने नसीब को कोसते
भर लायी थी पानी
आखिर नानी
जेठ की झूर दोपहरी में
भरने गयी थी नानी
नंगे पाँव
गङ्गलोडों से चढ़ते उतरते
अपने नसीब को कोसते
भर लायी थी पानी
आखिर नानी
बोली थी घुघुती
आँगन के अमुआ से
अकेली घर कुड़ी
नानी थी अब बुडी
आँखों से छलका था पानी
याद आई होगी
कोई पुरानी कहानी
ये घुघुती भी ना..
आँगन के अमुआ से
अकेली घर कुड़ी
नानी थी अब बुडी
आँखों से छलका था पानी
याद आई होगी
कोई पुरानी कहानी
ये घुघुती भी ना..
रेत सी जिन्दगी
फिसलती रही और वो समेटती रही
रोज एक पुल बनाती यादों के
और रोज वो जमीदोज हो जाता
और वो देखती रहती
दाद देता हूँ उसके हिम्मत की
फिसलती रही और वो समेटती रही
रोज एक पुल बनाती यादों के
और रोज वो जमीदोज हो जाता
और वो देखती रहती
दाद देता हूँ उसके हिम्मत की
आज नदी कुछ
सूनसान थी
उसे इन्तजार था उस फौंले का
उसके उस खालीपन का
जिसे उसे भरना था
पर आज न नानी थी
न फौंला
और नदी ...
सूनसान थी
उसे इन्तजार था उस फौंले का
उसके उस खालीपन का
जिसे उसे भरना था
पर आज न नानी थी
न फौंला
और नदी ...
पागल कवि
ऐ पागल कवि!!!!
क्यों लिखता है तू
भूख को
प्यास को
दर्द को
संवेदनाओं को
पगलिया गया है क्या??
लिख ना! लिख!!
उन आलीशान राज पथों को
राज महलों को
राज घरानों को
राज कुमारों को
सुनहरे रुपहले पर्दों को
क्यों लिखता है तू
भूख को
प्यास को
दर्द को
संवेदनाओं को
पगलिया गया है क्या??
लिख ना! लिख!!
उन आलीशान राज पथों को
राज महलों को
राज घरानों को
राज कुमारों को
सुनहरे रुपहले पर्दों को
क्यों लिखना है
फुटपाथ को
बलात्कार को
खुदकुशी को
अब भी सम्हल जा
अगर तुझे जिन्दा रहना है तो
लिख !!
धोखे को धोखे से
प्यार को आडम्बर से
इज्जत को उछाल कर
बड़ा पैसा है
इस धंधे में
ऐ कवि!!
बिकता क्यों नहीं
चुप रहता क्यों नहीं
कब तक पहनेगा इस खादी को
खुली आँखों से देखेगा बर्बादी को
तू तो वाकई पागल है
अरे! क्यों लिखता है
उन झुग्गी झोपड़ियों को
फूट चुकी खोपड़ियों को
मर चुके अरमानों को
रो रहे इमानों को
तुझे तो लिखना चाहिए
विकास के पथ को
खून की लथपथ को
सफ़ेद को
जलते चूल्हों को
सच लिखना छोड़ दे
तभी बचा पायेगा खुद के वजूद को
शर्त यही है कि
तू बिकने को तैयार हो
ऐ कवि...
फुटपाथ को
बलात्कार को
खुदकुशी को
अब भी सम्हल जा
अगर तुझे जिन्दा रहना है तो
लिख !!
धोखे को धोखे से
प्यार को आडम्बर से
इज्जत को उछाल कर
बड़ा पैसा है
इस धंधे में
ऐ कवि!!
बिकता क्यों नहीं
चुप रहता क्यों नहीं
कब तक पहनेगा इस खादी को
खुली आँखों से देखेगा बर्बादी को
तू तो वाकई पागल है
अरे! क्यों लिखता है
उन झुग्गी झोपड़ियों को
फूट चुकी खोपड़ियों को
मर चुके अरमानों को
रो रहे इमानों को
तुझे तो लिखना चाहिए
विकास के पथ को
खून की लथपथ को
सफ़ेद को
जलते चूल्हों को
सच लिखना छोड़ दे
तभी बचा पायेगा खुद के वजूद को
शर्त यही है कि
तू बिकने को तैयार हो
ऐ कवि...
"है ना"
बैठा करते थे
सगड़ के चारों तरफ
राफ़ लेने को
जो हाथों से हो कर
जाती थी जिगर तक
सगड़ के चारों तरफ
राफ़ लेने को
जो हाथों से हो कर
जाती थी जिगर तक
एक रजाई थी
जिसकी रुई सिमट गयी थी
गल गया था
कपड़ा
जो समेटे था
उन सबकी गरीबी को
जिसके बस में न था
अँधेरे को समेट पाना
पर वो फिर भी रजाई थी
जिसकी रुई सिमट गयी थी
गल गया था
कपड़ा
जो समेटे था
उन सबकी गरीबी को
जिसके बस में न था
अँधेरे को समेट पाना
पर वो फिर भी रजाई थी
एक तौली थी
पीतल की
जो पानी गर्म करने से ले कर
खाना पकाने तक का काम खुशी से कर लेती थी
सूनसान
मौन हो कर
आज के कूकरों की तरह चिल्लाती नहीं थी
हाँ उसके भात, दाल की खुशबू
फ़ैल जाती थी
पूरी बाखली में
पीतल की
जो पानी गर्म करने से ले कर
खाना पकाने तक का काम खुशी से कर लेती थी
सूनसान
मौन हो कर
आज के कूकरों की तरह चिल्लाती नहीं थी
हाँ उसके भात, दाल की खुशबू
फ़ैल जाती थी
पूरी बाखली में
एक थी चासनी
पूरे गाँव की साज्जी
जो धुलती थी
ब्या बरात
नवान पर
तब होती थी
सरसों
और उसका पिरपिरी फैलाता तेल
पूड़ियाँ उछलती कूदती थीं
और उनकी धूंगार फ़ैल जाती थी पूरे गाँव में
आज तो है रिफाइंड
न सुगंध न दुर्गन्ध
आज के अचेतन हो चुके रिश्तों की तरह
पूरे गाँव की साज्जी
जो धुलती थी
ब्या बरात
नवान पर
तब होती थी
सरसों
और उसका पिरपिरी फैलाता तेल
पूड़ियाँ उछलती कूदती थीं
और उनकी धूंगार फ़ैल जाती थी पूरे गाँव में
आज तो है रिफाइंड
न सुगंध न दुर्गन्ध
आज के अचेतन हो चुके रिश्तों की तरह
एक था विश्वास
जो हुआ करता था
हर दिल में
हर घर में
नहीं होती थी
ताला कुच्ची।
चूल्हा किसी का
जो हुआ करता था
हर दिल में
हर घर में
नहीं होती थी
ताला कुच्ची।
चूल्हा किसी का
आग किसी की
ऐंचा पैंचा
दिलों से लेकर नून तेल तक
बहुत आसान था जीना
आज सब कुछ है
पर विश्वास नहीं
लिपी पुती देहों
दिखावे के भावों
से ढका आवरण
जिन्दा होने का ढोंग करते पुतले
है ना जिन्दगी की जद्दोजहद
ऐंचा पैंचा
दिलों से लेकर नून तेल तक
बहुत आसान था जीना
आज सब कुछ है
पर विश्वास नहीं
लिपी पुती देहों
दिखावे के भावों
से ढका आवरण
जिन्दा होने का ढोंग करते पुतले
है ना जिन्दगी की जद्दोजहद
गांव के पंख
गाँव की चौपालें
बदलने लगी हैं
राजनीति का जहर असर कर रहा है
अब फसक हो रहे हैं
सह और मात के
तोड़ने और जोड़ने के
बदलने लगी हैं
राजनीति का जहर असर कर रहा है
अब फसक हो रहे हैं
सह और मात के
तोड़ने और जोड़ने के
सीमेंट के रास्तों से पट चुके है गाँव
दूब सिकुड़ती जा रही है
टूटते जा रहे हैं
घर
बनती जा रही हैं
दीवारें
दूब सिकुड़ती जा रही है
टूटते जा रहे हैं
घर
बनती जा रही हैं
दीवारें
हो रहा विकास
बढ़ रही प्यास
पैसों की
सूखे की चपेट में हैं रिश्ते
अकाल है भावों का
बढ़ रही प्यास
पैसों की
सूखे की चपेट में हैं रिश्ते
अकाल है भावों का
बहुत बदल गया है गाँव
शहर को देख कर
बाजार को घर ले आया है गाँव
खुद बिकने को तैयार बैठा है
हर हाल में
हरी घास भी
खरीद लाये हैं
शहर वाले
शहर को देख कर
बाजार को घर ले आया है गाँव
खुद बिकने को तैयार बैठा है
हर हाल में
हरी घास भी
खरीद लाये हैं
शहर वाले
अब सन्नाटा है
चौपालों में
अब दहाड़ रही है राजनीति
घर घर
चूल्हों में आग नहीं है
हाँ, मुँह उगल रहे हैं
आग
सिक रहा भोला भाला गाँव
चौपालों में
अब दहाड़ रही है राजनीति
घर घर
चूल्हों में आग नहीं है
हाँ, मुँह उगल रहे हैं
आग
सिक रहा भोला भाला गाँव
बाँट दिए हैं
छाँट दिए हैं
मेलों में मिलना होता है
वोटों को बाँटने और काटने के लिए
छद्म वेशों
में घुस चुके हैं
गाँव के हर घर में
जन-जन तक
और मनों को कुत्सित कर चुकी है
आज की कुत्सित राजनीति
यों ही चलता रहा तो
मिट जायेगा
गाँव और गाँव का वजूद
फिर ढूँढने जायेंगे किसी
गाँव को
शहर की गलियों में
छाँट दिए हैं
मेलों में मिलना होता है
वोटों को बाँटने और काटने के लिए
छद्म वेशों
में घुस चुके हैं
गाँव के हर घर में
जन-जन तक
और मनों को कुत्सित कर चुकी है
आज की कुत्सित राजनीति
यों ही चलता रहा तो
मिट जायेगा
गाँव और गाँव का वजूद
फिर ढूँढने जायेंगे किसी
गाँव को
शहर की गलियों में
जाना ही होगा
बेटा! जा रहा
हाँ, इजा जाना ही होगा
जाने का मन तो नहीं
पर जाना ही होगा
यहाँ रह कर भी तो पूरा नहीं पड़ेगा
बहिन की शादी भी तो करनी है
तेरी आँखों में जो मोतियाबिंद पड़ गया है
वो भी तो पकने वाला है
उसका इलाज......
बाबू की खाँसी भी तो बढ़ने लगी है
हुक्का नहीं दीखता अब हाथों में
कैसे न जाऊं ईजा
कब तक हाथ फैलाना होगा
नून तेल के लिए
बिरादरी के ताने
मैं नहीं सुन सकता अब
किताबों को पढ़कर भी क्या करूँ
हाथ और दिमाग का द्वंद्व
अब देखा नहीं जाता
बैल बेच देना
बस एक गाय पाल लेना
चाय रँगने को कब तक पेंचा लेते रहेंगे
बेटा बैल.......
लोग क्या कहेंगे
बंजर खेत मुझसे नहीं देखे जायेंगे
ईजा देख खेत ही नहीं
घरों के आँगन भी तो बंजी गए हैं
उग आयी है घास तालों में
कुच्ची साथ ले गए
दिल्ली, बम्बई वाले
ईजा पहाड़ की कुच्ची वहीँ तो है
हाँ ईजा! तूने सही कहा
जा जा
हम तो यही हुए
यहीं रहे
यहीं मरेंगे
तू सुधार अपना जीवन
ले ईजा
ये खजुरे, खिररखाजे
सिंगल, बेड्यां पू
तुझे भूख लगेगी बाटे में
जा ईजा जा
फलना-फूलना
लौ बेग आना
हाँ इजा जाना ही होगा
आखिर मुझे भी तो
बड़ा आदमी बनना है
छोड़ना ही पड़ता है घर
एक नया घर बसाने के लिए
इजा जा
जाते ही फोन कर देना
जिसके सहारे जी लेंगे हम
समय ही तो काटना है
इजा
और तो .......हाँ, इजा जाना ही होगा
जाने का मन तो नहीं
पर जाना ही होगा
यहाँ रह कर भी तो पूरा नहीं पड़ेगा
बहिन की शादी भी तो करनी है
तेरी आँखों में जो मोतियाबिंद पड़ गया है
वो भी तो पकने वाला है
उसका इलाज......
बाबू की खाँसी भी तो बढ़ने लगी है
हुक्का नहीं दीखता अब हाथों में
कैसे न जाऊं ईजा
कब तक हाथ फैलाना होगा
नून तेल के लिए
बिरादरी के ताने
मैं नहीं सुन सकता अब
किताबों को पढ़कर भी क्या करूँ
हाथ और दिमाग का द्वंद्व
अब देखा नहीं जाता
बैल बेच देना
बस एक गाय पाल लेना
चाय रँगने को कब तक पेंचा लेते रहेंगे
बेटा बैल.......
लोग क्या कहेंगे
बंजर खेत मुझसे नहीं देखे जायेंगे
ईजा देख खेत ही नहीं
घरों के आँगन भी तो बंजी गए हैं
उग आयी है घास तालों में
कुच्ची साथ ले गए
दिल्ली, बम्बई वाले
ईजा पहाड़ की कुच्ची वहीँ तो है
हाँ ईजा! तूने सही कहा
जा जा
हम तो यही हुए
यहीं रहे
यहीं मरेंगे
तू सुधार अपना जीवन
ले ईजा
ये खजुरे, खिररखाजे
सिंगल, बेड्यां पू
तुझे भूख लगेगी बाटे में
जा ईजा जा
फलना-फूलना
लौ बेग आना
हाँ इजा जाना ही होगा
आखिर मुझे भी तो
बड़ा आदमी बनना है
छोड़ना ही पड़ता है घर
एक नया घर बसाने के लिए
इजा जा
जाते ही फोन कर देना
जिसके सहारे जी लेंगे हम
समय ही तो काटना है
इजा
समय बदलेगा
पलट कर देख तो लेते
बोलते न सही
जुबाँ तो उनकी भी अटकी थी
और तूम्हारी भटकी है
यों कोई चोर उचक्का तो न था
जिसे तुमने नकारना उचित समझा
बोलते न सही
जुबाँ तो उनकी भी अटकी थी
और तूम्हारी भटकी है
यों कोई चोर उचक्का तो न था
जिसे तुमने नकारना उचित समझा
लाशों को चीखने देना
उनकी चीख को दबाने के लिए
खुद जोर से चीखना
और फिर मौन साध लेना
क्या यही हैं
दावे
पेट को भर देने के
हाथों को काम देने के
उनकी चीख को दबाने के लिए
खुद जोर से चीखना
और फिर मौन साध लेना
क्या यही हैं
दावे
पेट को भर देने के
हाथों को काम देने के
रहम करो
इन गिरगिटी चालों को बन्द करो
सड़कों और फुटपाथों को
जीने दो
झोपड़ियों को चिंगारी मत दिखाओ
बंद नालियों के कीड़े भी काम के होते हैं
जो तुम्हारी गन्दगी को छुपाते हैं
दिमागी कीड़े से
कहीं ज्यादा समझदार होते हैं
इन गिरगिटी चालों को बन्द करो
सड़कों और फुटपाथों को
जीने दो
झोपड़ियों को चिंगारी मत दिखाओ
बंद नालियों के कीड़े भी काम के होते हैं
जो तुम्हारी गन्दगी को छुपाते हैं
दिमागी कीड़े से
कहीं ज्यादा समझदार होते हैं
तोतों को मत सिखाओ
राम राम रटना
एक दिन यही तोते मरा मरा कहेंगे
और तुम
भीख मांगोगे जिन्दगी की
राम राम रटना
एक दिन यही तोते मरा मरा कहेंगे
और तुम
भीख मांगोगे जिन्दगी की
याद रखना
आग जब लगती है तो
हवा का रूख ही बहुत होता है
भस्म हो जाओगे
एक माचिस की तिल्ली से
तब ढूँढोगे दरिया
और वो सूख चूका होगा
और आग बह रही होगी
आग जब लगती है तो
हवा का रूख ही बहुत होता है
भस्म हो जाओगे
एक माचिस की तिल्ली से
तब ढूँढोगे दरिया
और वो सूख चूका होगा
और आग बह रही होगी
डॉमत करो बात
सभ्यता और संस्कृति की
अपनी माटी और थाती की
बाजार से खरीद कर नहीं सहेजी जा सकती संस्कृति
कहाँ गया तुम्हारा हुड़का
दमूं
देंन दमू बुं दमुं
भूल गए ना
झोड़ा चाँचरी
बन गीत
बग्वाल के वीर गान
फोड़ दिया हुड़का
जाती के सर पर
जोड़ दिया ढोल
जाती के पोल पर
और बताते हो
खुद को रक्षक
कहाँ है तुम्हारी संस्कृति
कभी सुनो हुड़के का आर्तनाद
दमूं का मौन
मजाक उड़ाने के शिवा क्या किया
माना नाली दिया तो क्या दिया
एक सुपा धान क्या दिया बन बैठे पधान
गड़े भीड़ों को खुदवा कर
मै हल हलभणि को छिड़वा कर
घर के देहली पर ही
छोड़ा डाल कर
खुद विष्णु कहलाने वाले
क्या बचाएंगे संस्कृति
सभ्यता और संस्कृति की
अपनी माटी और थाती की
बाजार से खरीद कर नहीं सहेजी जा सकती संस्कृति
कहाँ गया तुम्हारा हुड़का
दमूं
देंन दमू बुं दमुं
भूल गए ना
झोड़ा चाँचरी
बन गीत
बग्वाल के वीर गान
फोड़ दिया हुड़का
जाती के सर पर
जोड़ दिया ढोल
जाती के पोल पर
और बताते हो
खुद को रक्षक
कहाँ है तुम्हारी संस्कृति
कभी सुनो हुड़के का आर्तनाद
दमूं का मौन
मजाक उड़ाने के शिवा क्या किया
माना नाली दिया तो क्या दिया
एक सुपा धान क्या दिया बन बैठे पधान
गड़े भीड़ों को खुदवा कर
मै हल हलभणि को छिड़वा कर
घर के देहली पर ही
छोड़ा डाल कर
खुद विष्णु कहलाने वाले
क्या बचाएंगे संस्कृति
सुनो
ये हुड़के
ढोल
दमाऊ न बचे तो
क्या ख़ाक बचेगी ये
तुम्हारी ढ़कोसले वाली संस्कृति
इधर उधर डोलती सभ्यता
जिस दिन मैं
बजाना सीखूंगा हुड़का
ठोकुंगा दमाऊं की ताल
थिरकुंगा छलिया बन कर
न जाति का भेद होगा
न बन्धन
तब महकेगी सभ्यता
और उन्मुक्त हो कर नृत्य करेगी संस्कृति
ये हुड़के
ढोल
दमाऊ न बचे तो
क्या ख़ाक बचेगी ये
तुम्हारी ढ़कोसले वाली संस्कृति
इधर उधर डोलती सभ्यता
जिस दिन मैं
बजाना सीखूंगा हुड़का
ठोकुंगा दमाऊं की ताल
थिरकुंगा छलिया बन कर
न जाति का भेद होगा
न बन्धन
तब महकेगी सभ्यता
और उन्मुक्त हो कर नृत्य करेगी संस्कृति
बहुत दूर जा चुके हो
जब से तू
खुदा हुआ
सब से तू
जुदा हुआ
नाप ली
जिंदगी तूने
आज तू
आज तू
बेहुदा हुआ
प्यासा है
खून का तू
खुद से
खुद से
गुमशुदा हुआ
पथ-लथपथ
तेरे और मेरे बीच की
दूरियाँ अनन्त हैं
एक ऐसी मृग मरीचिका
जिसे आँखें आज तक पीने को आतुर हैं
दिल छोड़ने को राजी नहीं
मन के घोड़े
हिनहिना रहे हैं
मानो जंग में जीत नजदीक आ खड़ी हो
विजय श्री
विजय गान गा रही हो
दूरियाँ अनन्त हैं
एक ऐसी मृग मरीचिका
जिसे आँखें आज तक पीने को आतुर हैं
दिल छोड़ने को राजी नहीं
मन के घोड़े
हिनहिना रहे हैं
मानो जंग में जीत नजदीक आ खड़ी हो
विजय श्री
विजय गान गा रही हो
आज भी सबेरा हुआ
सूरज उसी पहाड़ी की छोर से चढ़ा
जहाँ से चढ़ता है
है ना कितना सुन्दर
स्वतंत्रता के गीत गाते पाहन
रात के आगोश से
मुक्त होते स्वप्न
निकल पड़े हैं
परिंदों के मानिन्द
सूरज उसी पहाड़ी की छोर से चढ़ा
जहाँ से चढ़ता है
है ना कितना सुन्दर
स्वतंत्रता के गीत गाते पाहन
रात के आगोश से
मुक्त होते स्वप्न
निकल पड़े हैं
परिंदों के मानिन्द
ज्यों ज्यों दिन चढ़ा
सम्पूर्ण क्षितिज में जहर घुलता गया
चहुँ ओर तीर बरछी कटार
से टकराते शब्द
सफेदपोश मगरमच्छ
मदमस्त घड़ियाल
कर रहे हैं
बिष वमन
एक गुबार जो फ़ैल गया है
जिसमें लिपटे हैं
जाति संप्रदाय के मुद्दे
जो अश्रु गैस सी है
उस समाज के लिए
जिसने आज चुनना है
रावण और कुम्भकर्ण में से एक को
सम्पूर्ण क्षितिज में जहर घुलता गया
चहुँ ओर तीर बरछी कटार
से टकराते शब्द
सफेदपोश मगरमच्छ
मदमस्त घड़ियाल
कर रहे हैं
बिष वमन
एक गुबार जो फ़ैल गया है
जिसमें लिपटे हैं
जाति संप्रदाय के मुद्दे
जो अश्रु गैस सी है
उस समाज के लिए
जिसने आज चुनना है
रावण और कुम्भकर्ण में से एक को
लोहे तांबे सोने और चाँदी से
मढ़े महिमा के गीत
बिलख रहे हैं
कहीं तहखाने में जा छुपे हैं
और कुछ झूल रहे हैं
सत्ता के गलियारों में
कुछ आक्रोशित हो
आत्महत्या कर चुके
कुछ दुबारा साँस लेने की सोच रहे हैं
यही है प्रगति पथ
यही है सत्पथ
लथपथ लथपथ लथपथ
मढ़े महिमा के गीत
बिलख रहे हैं
कहीं तहखाने में जा छुपे हैं
और कुछ झूल रहे हैं
सत्ता के गलियारों में
कुछ आक्रोशित हो
आत्महत्या कर चुके
कुछ दुबारा साँस लेने की सोच रहे हैं
यही है प्रगति पथ
यही है सत्पथ
लथपथ लथपथ लथपथ
विकास आ रहा है या
विकास आ रहा है
मैंने भी सुना
तुमने भी सुना होगा
पहाड़ के गाँवों से विकास जा रहा है
बड़ी अजीब बात है ना
लेकिन यही सच है
रोडो के जाल बिछे हैं
घर घर स्कूल खुले हैं
सत्य है
पर मित्रो पहाड़ अंदर से दरक रहे हैं
और लोग शहर को फरक रहे हैं
यह भी कटु सत्य है
बह रहा है पैसा
उग रहा है रुपया
दैवीय आपदा का जुमला कारगर है
और रुपये उगाने की खाद भी
गाड़ गधेरे नौले
अछेटी गए हैं
नयी सड़कों के मलवे से
एक सड़क जो
एक दशक पहले शुरू हुई थी
आज तक पडी है
अर्धचेतना अवस्था में
न प्राण देने वाला कोई
न प्राण हरने वाला कोई
गाँव के स्कूल
अब शाम को बन जाते हैं
शराबियों कबाबियों के अड्डे
क्या कहेंगे आप
मैंने भी सुना
तुमने भी सुना होगा
पहाड़ के गाँवों से विकास जा रहा है
बड़ी अजीब बात है ना
लेकिन यही सच है
रोडो के जाल बिछे हैं
घर घर स्कूल खुले हैं
सत्य है
पर मित्रो पहाड़ अंदर से दरक रहे हैं
और लोग शहर को फरक रहे हैं
यह भी कटु सत्य है
बह रहा है पैसा
उग रहा है रुपया
दैवीय आपदा का जुमला कारगर है
और रुपये उगाने की खाद भी
गाड़ गधेरे नौले
अछेटी गए हैं
नयी सड़कों के मलवे से
एक सड़क जो
एक दशक पहले शुरू हुई थी
आज तक पडी है
अर्धचेतना अवस्था में
न प्राण देने वाला कोई
न प्राण हरने वाला कोई
गाँव के स्कूल
अब शाम को बन जाते हैं
शराबियों कबाबियों के अड्डे
क्या कहेंगे आप
आज भी मीलों
मरीज लाये जाते हैं
डोलियों में कन्धों के सहारे
कुछ किस्मत से जिन्दे पहुँच जाते हैं शहर
कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ने को विवश
मरीज लाये जाते हैं
डोलियों में कन्धों के सहारे
कुछ किस्मत से जिन्दे पहुँच जाते हैं शहर
कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ने को विवश
आज भी बनती और
बंटती है
और उजाड़ रही है कच्ची शराब
और हम दम ठोक रहे हैं
विकास विकास
विकास हुआ है
कुछ चंद विकसित लोगों का
मैं ये भी नहीं कह रहा विकास नहीं हो रहा है
हो रहा है
पर विकास कम विनाश ज्यादा
असन्तुलित भौतिक विकास
नहीं हुआ हमारी नैतिकता
और हमारे विचारों का विकास
हम ज्यादा संकीर्ण हुए हैं
पहले से अब
बंटती है
और उजाड़ रही है कच्ची शराब
और हम दम ठोक रहे हैं
विकास विकास
विकास हुआ है
कुछ चंद विकसित लोगों का
मैं ये भी नहीं कह रहा विकास नहीं हो रहा है
हो रहा है
पर विकास कम विनाश ज्यादा
असन्तुलित भौतिक विकास
नहीं हुआ हमारी नैतिकता
और हमारे विचारों का विकास
हम ज्यादा संकीर्ण हुए हैं
पहले से अब
हो गयी कुर्की
खेतों में खड़ी फसल
न जाने कब धराशायी हो गयी
और कब बैंकों के नोटिस
चस्पा हो गये घर के दरवाजों पर
क्योंकि पढ़ना नहीं जानता
दरवाजा
न जाने कब धराशायी हो गयी
और कब बैंकों के नोटिस
चस्पा हो गये घर के दरवाजों पर
क्योंकि पढ़ना नहीं जानता
दरवाजा
घर का चूल्हा
आज रात बुझा कर सोई
सुबह जलाने के लिए
देखा सामने नीम के पेड़ से
लटकी थी एक लाश
अब उस लाश को जलाये या
चूल्हा
आज रात बुझा कर सोई
सुबह जलाने के लिए
देखा सामने नीम के पेड़ से
लटकी थी एक लाश
अब उस लाश को जलाये या
चूल्हा
सब कुछ बेच कर भी
नहीं बचा पाई देह को
घासलेट की दुर्गन्ध
मिल गयी थी
देह और केशों की
सर चढ़ती जली अधजली
दुर्गन्ध से
नहीं बचा पाई देह को
घासलेट की दुर्गन्ध
मिल गयी थी
देह और केशों की
सर चढ़ती जली अधजली
दुर्गन्ध से
बच्चे ढ़ूँढ रहे थे
राख के ढेर में हड्डियाँ
कुछ कर रहे थे कारवाई
कुर्की की
खेत में बचे खुचे गन्ने के डंठलों की
खपरैल से ढकीं
झोपडी की
घास फूस से बनी मढ़याँ की
राख के ढेर में हड्डियाँ
कुछ कर रहे थे कारवाई
कुर्की की
खेत में बचे खुचे गन्ने के डंठलों की
खपरैल से ढकीं
झोपडी की
घास फूस से बनी मढ़याँ की
खुश था महाजन
गिरवी में मिले जेवरातों को हड़प कर
हिस्से की आस में
और भी किस्से गढ़ रहे है
बहा रहे हैं घड़ियाली आँशू
अब आँगन का आम नीम
सब नीलाम हो चुके
बस परिंदे आज भी आजाद हैं
ये खुशी की बात है
गिरवी में मिले जेवरातों को हड़प कर
हिस्से की आस में
और भी किस्से गढ़ रहे है
बहा रहे हैं घड़ियाली आँशू
अब आँगन का आम नीम
सब नीलाम हो चुके
बस परिंदे आज भी आजाद हैं
ये खुशी की बात है
मौसम की तरह
देखा
मैं कहता था ना
तू भी एक दिन मौसम की तरह बदल जाएगा
कल तू बदला था
आज मौसम भी बदल गया
तूने तो मौसम को भी मात दे दी
मौक़ा ही नहीं दिया
इस गरीब को
मौसम की मार झेलने को
घिर आया है
बादल उमड़ घुमड़ कर
जैसे तेरी उलाहनाओं ने पहरा दिया था
मेरी नींद पर
सपने तो कांपने लगे थे
मौसम और तुम एक जैसे ही तो हो
है ना सही बात
मैं कहता था ना
तू भी एक दिन मौसम की तरह बदल जाएगा
कल तू बदला था
आज मौसम भी बदल गया
तूने तो मौसम को भी मात दे दी
मौक़ा ही नहीं दिया
इस गरीब को
मौसम की मार झेलने को
घिर आया है
बादल उमड़ घुमड़ कर
जैसे तेरी उलाहनाओं ने पहरा दिया था
मेरी नींद पर
सपने तो कांपने लगे थे
मौसम और तुम एक जैसे ही तो हो
है ना सही बात
मौन भी चीखता है
अरे!! तुम्हें जश्न के ढोल खूब सुनाई देते
हैं
कभी मौन हो चुके
दर्द के क्रन्दन को सुनो
जो फाड़ देगा कान के पर्दे
दहला देगा दिल को
कभी मौन हो चुके
दर्द के क्रन्दन को सुनो
जो फाड़ देगा कान के पर्दे
दहला देगा दिल को
अरे चमचमाते जगमगाते चौराहों को देख लेते हो
कभी उन कोठरियों को भी
देख लो
जिनके दिए बुझ चुके हैं
तुम्हारी पैदा की गयी काल्पनिक
आँधियों से
कभी उन कोठरियों को भी
देख लो
जिनके दिए बुझ चुके हैं
तुम्हारी पैदा की गयी काल्पनिक
आँधियों से
बहुत पलट लिए हैं पन्ने
रच दिए हैं इतिहास
नाप लिए हैं भूगोल
जरा समाज शास्त्र को भी तो देख लो
जिस अर्थ की बात करते हो
क्या वह सार्थक है
निरर्थक हो चुके मौन की व्यथा को सुन लो
जो चीख रहा है
डेंगू का मच्छर बनते देर नहीं लगेगी
सुन लो!!!!!
रच दिए हैं इतिहास
नाप लिए हैं भूगोल
जरा समाज शास्त्र को भी तो देख लो
जिस अर्थ की बात करते हो
क्या वह सार्थक है
निरर्थक हो चुके मौन की व्यथा को सुन लो
जो चीख रहा है
डेंगू का मच्छर बनते देर नहीं लगेगी
सुन लो!!!!!
कराह रही है आत्मा
इन फूलों, फूल मालाओं
गुलदस्तों
और शब्दाडंबरो के बोझ तले
दबकर
पुकार रही है आत्मा
बचालो मुझे
इन दोगले चरित्रों से
आगे बढ़ कर
उठ रहीं हैं
अंगुलियाँ मेरे होने और न होने के
प्रश्नों पर
दुत्कार रही है आत्मा
स्वाभिमान के लुट जाने
और घड़ियाली आँसू बहाने पर
सुन लो ठहर कर
वो जाने वालो
मत कुचलो
मत करो सुनी की अनसुनी
मत दबाओ आत्मा की आवाज को
मंच से नहीं बोलती आत्मा
बोलती हैं
महत्वाकांक्षाओ के बड़े बोल
आज अगर बिना सुने
बोलने गए तो समझ लेना
सुनने वाले बचेंगे नहीं
अब सब कुछ तेरे हाथ में है
इन फूलों, फूल मालाओं
गुलदस्तों
और शब्दाडंबरो के बोझ तले
दबकर
पुकार रही है आत्मा
बचालो मुझे
इन दोगले चरित्रों से
आगे बढ़ कर
उठ रहीं हैं
अंगुलियाँ मेरे होने और न होने के
प्रश्नों पर
दुत्कार रही है आत्मा
स्वाभिमान के लुट जाने
और घड़ियाली आँसू बहाने पर
सुन लो ठहर कर
वो जाने वालो
मत कुचलो
मत करो सुनी की अनसुनी
मत दबाओ आत्मा की आवाज को
मंच से नहीं बोलती आत्मा
बोलती हैं
महत्वाकांक्षाओ के बड़े बोल
आज अगर बिना सुने
बोलने गए तो समझ लेना
सुनने वाले बचेंगे नहीं
अब सब कुछ तेरे हाथ में है
मत कर दिल हल्का
ये वक्त भी तेरा ही है
जिसे आज तू अपना नहीं पा रहा होगा
यही वक्त है
जो तुझे और मजबूत बनाएगा
ये अमावस्या
पूर्णिमा के आने का संकेत हैं
जब चाँद होगा
पूरे शबाब में
और तेरा निर्मल मन
होगा शरद का आकाश
तुझे मिलेगा
जो चाहिए
बस जुट जा और मजबूती के साथ
धार दे अपने
वर्तमान को
भविष्य तेरा होगा
खुद आएगा तेरा वरण करने
बस तू वर्तमान को वरण कर
बदलना होगा
जातियाँ खूब बोलने लगी हैं।
बिलबिलाने, मिमियाने, चीखने-चिल्लाने
लगी हैं
टिकट की खिड़कियों
गाँव की पंचायतों
विधानसभाओं और संसद के गलियारों में
बेसुध अलग अलग पंक्तियों में खड़ी हैं जातियाँ
अपने अपने तर्क लिये
हरा नीला पीला लाल केसरिये रंगों को
अपना बना
झंडे लेकर निकल पडी हैं जातियाँ
लेकर रहेंगे
अपना हक़ हुक़ूक़
अब नहीं दबेंगे
एक एक कर फन उठाने लगी हैं जातियाँ
बिलबिलाने, मिमियाने, चीखने-चिल्लाने
लगी हैं
टिकट की खिड़कियों
गाँव की पंचायतों
विधानसभाओं और संसद के गलियारों में
बेसुध अलग अलग पंक्तियों में खड़ी हैं जातियाँ
अपने अपने तर्क लिये
हरा नीला पीला लाल केसरिये रंगों को
अपना बना
झंडे लेकर निकल पडी हैं जातियाँ
लेकर रहेंगे
अपना हक़ हुक़ूक़
अब नहीं दबेंगे
एक एक कर फन उठाने लगी हैं जातियाँ
और बाँटो रेवड़ियाँ
एक दिन तुम्हें ही बाँट कर खा जाएँगी जातियाँ
बहुत शौक है कुर्सियों का
हर एक पाये को सम्हाले है
एक नहीं सैकड़ों जातियाँ
माँगो बोट
बाँटो नोट
अब नहीं बिकने और डिगने वाली हैं ये जातियाँ
एक दिन तुम्हें ही बाँट कर खा जाएँगी जातियाँ
बहुत शौक है कुर्सियों का
हर एक पाये को सम्हाले है
एक नहीं सैकड़ों जातियाँ
माँगो बोट
बाँटो नोट
अब नहीं बिकने और डिगने वाली हैं ये जातियाँ
मंदिरों मस्जिदों
गुरुद्वारों को मत बनाओ अखाड़ा
गरीब के पेट को मत बनाओ जरिया
कब तक बाँटोगे
कहीं ये देश ही न बाँट दें ये जातियाँ
गुरुद्वारों को मत बनाओ अखाड़ा
गरीब के पेट को मत बनाओ जरिया
कब तक बाँटोगे
कहीं ये देश ही न बाँट दें ये जातियाँ
तुम्हारे पास है
अकूत खजाना
और मनमाना है
तुमने खरीद ली हैं लाठियाँ
खाकी वर्दियाँ
लपलपाते कोड़े
क्या फिर भी तोड़ पाओगे
इन विद्रोही आवाजों को
जो उठ रही है
चीख रही हैं चिल्ला रही हैं
अब तो निकल पड़ी हैं जातियाँ
अकूत खजाना
और मनमाना है
तुमने खरीद ली हैं लाठियाँ
खाकी वर्दियाँ
लपलपाते कोड़े
क्या फिर भी तोड़ पाओगे
इन विद्रोही आवाजों को
जो उठ रही है
चीख रही हैं चिल्ला रही हैं
अब तो निकल पड़ी हैं जातियाँ
अब भी जाग जाओ
तोड़ डालो तुष्टिकरण के भँवर को
देखो गरीब को
गरीबखाने को
क्या नहीं हो सकता यह देश
जातियों के विष से अलग
जहाँ हो केवल और केवल
मानवता
तोड़ डालो तुष्टिकरण के भँवर को
देखो गरीब को
गरीबखाने को
क्या नहीं हो सकता यह देश
जातियों के विष से अलग
जहाँ हो केवल और केवल
मानवता
क्या ये है बचपन
कूड़ा बिन रहा था
कुछ अद्धे पव्वों
और बोतलों से बूँद-बूँद इकट्ठा कर रहा था
कुछ नशे में लग रहा था
और नशे के ही जुगाड़ में लगा हुआ था
आँखों में मजबूरी
कंधे पर टंगा मैला कुचैला एक बोरा
जिसमें बजबजा रहे थे अरमान
उसने सपने देखना सीखा ही नहीं
क्योंकि वो सोता है फुटपाथ पर
जहाँ सपने देखना सख्त मना है
सोता है रोज
पर जागने के लिए नहीं
उसे रोज सुनाई देती है
स्कूल की घंटी
उसके लिए वो होता है
कूड़े दान को उलटने का समय
पूछने पर बोला
अंकल मुझे किताबों से क्या करना
पेट पहले
फिर परिवार
मन करता है
मैं भी जाऊँ स्कूल
पर अंकल..........
चल पड़ता है आगे को
लड़खड़ाते हुए
कुछ अद्धे पव्वों
और बोतलों से बूँद-बूँद इकट्ठा कर रहा था
कुछ नशे में लग रहा था
और नशे के ही जुगाड़ में लगा हुआ था
आँखों में मजबूरी
कंधे पर टंगा मैला कुचैला एक बोरा
जिसमें बजबजा रहे थे अरमान
उसने सपने देखना सीखा ही नहीं
क्योंकि वो सोता है फुटपाथ पर
जहाँ सपने देखना सख्त मना है
सोता है रोज
पर जागने के लिए नहीं
उसे रोज सुनाई देती है
स्कूल की घंटी
उसके लिए वो होता है
कूड़े दान को उलटने का समय
पूछने पर बोला
अंकल मुझे किताबों से क्या करना
पेट पहले
फिर परिवार
मन करता है
मैं भी जाऊँ स्कूल
पर अंकल..........
चल पड़ता है आगे को
लड़खड़ाते हुए
भीड़ का हिस्सा हूँ
डिग्रियों के पुलिंदे लिए
निकल पड़ा हूँ
सड़क पर
भीड़ के पीछे
भीड़ बन कर
शायद ये मेरी मजबूरी है
निकल पड़ा हूँ
सड़क पर
भीड़ के पीछे
भीड़ बन कर
शायद ये मेरी मजबूरी है
डिग्रियाँ खरीदने वाले
खरीद सकते हैं
नौकरियाँ भी
मनमाफिक
सरकारी काउंटरों से
खरीद सकते हैं
नौकरियाँ भी
मनमाफिक
सरकारी काउंटरों से
हाथ काँप रहे हैं
पैर लड़खड़ा रहे हैं
अंतहीन पंक्तियों को देख कर
कुछ खिड़कियाँ बंद हैं
जिनके दरवाजे आभासी तौर पर बंद हैं
मेरे लिए
क्योंकि मेरे पास नहीं हैं
गड्डियाँ फिजूल की
पैर लड़खड़ा रहे हैं
अंतहीन पंक्तियों को देख कर
कुछ खिड़कियाँ बंद हैं
जिनके दरवाजे आभासी तौर पर बंद हैं
मेरे लिए
क्योंकि मेरे पास नहीं हैं
गड्डियाँ फिजूल की
फिर भी खड़ा हूँ
एक आशा के साथ
कोई तो होगा
पैसों के बागों के बीच
आम लगाने वाला माली
कभी तो आएगा मेरा भी वक्त
जब होगा मेरे हाथों में
काम
एक आशा के साथ
कोई तो होगा
पैसों के बागों के बीच
आम लगाने वाला माली
कभी तो आएगा मेरा भी वक्त
जब होगा मेरे हाथों में
काम
बदल गया
छांस की खकोड़ा खकोड़
नहीं आती अब सुनने में
धिनाली अब नहीं पूछी जाती
भेंट होने पर
और नाली अब ढूंढनी
पड़ती है
भाड़ के भकारों में
माने का मान
अब नहीं चलता
घर के ऐंचे-पैंचे में
नहीं आती अब सुनने में
धिनाली अब नहीं पूछी जाती
भेंट होने पर
और नाली अब ढूंढनी
पड़ती है
भाड़ के भकारों में
माने का मान
अब नहीं चलता
घर के ऐंचे-पैंचे में
बैलों को सिंगारने का शौक
अब कहाँ
कलकुत्ते से नहीं बनते अब सिंगोडे
नहीं घनघनाते घाणे खांकर
खरकों के गोठों में
घरों में एक मैंस एक भैंस
न हल्द न बल्द
न ख़ुर्सानी न किसानी
गाँव की हवा कुछ है अब अनजानी
अब कहाँ
कलकुत्ते से नहीं बनते अब सिंगोडे
नहीं घनघनाते घाणे खांकर
खरकों के गोठों में
घरों में एक मैंस एक भैंस
न हल्द न बल्द
न ख़ुर्सानी न किसानी
गाँव की हवा कुछ है अब अनजानी
बदलाव
खुर्दरी हथेलियाँ
बहुत कुछ बोल देती थीं
अब तो इनमें
खुर्दरापन है ही नहीं
वो आग
जो वर्षो पहले
जलाती थीं
घर के चूल्हे
हाथ का हथिन्डा
वो कुल्हाड़ी का बिंडा
हल और हलभाणी
वो बल्द की घाँड़ी
वो रामी वो बौराणी
टांडी भांडी
सब स्तब्ध है
खर्क की धुरानी में ध्वांर खा रही है।
इन नरम हाथों को
इनकी जरूरत अब कहाँ
अब तो पोशे की
दुर्गन्ध
दूध के गिलास तक नहीं आती
अब आँगन के किनारे माल्टा, नारंगी, कहाँ
सीमेंट से बूझ दिये गए है दुले
अन्दर ही अन्दर
घुट रही है
दूब और चलमोड़ी
स्याप, मूसे, छीपाड़े, ग्वाण
ये सब तो
अब हम खुद बन चुके हैं
भीड़ों में
घास नहीं उगती
उगती हैं
मन की दूरियाँ
भीड़े बाँट रही हैं हमको
घर की
देहलियों में ऐपण
नकली चिपकने लगे हैं
तुलसी एक डिब्बे में सिमट गयी है
जैसे बूढ़ापा एक कमरे में
पड़ोस से धिनाली का पैना
अब नहीं चलता
दूध बिकता है
गांव का गाँव में
अब आने बाणे
नहीं सुनाती आमा
सुनाये भी किसे
नाती मस्त है
शिनचेन, डोरेमोन
मोटू पतलू के माया जाल में
अब हुक्का लिए
बूबू नहीं लगाते धात
और फटकार
लिटवा नहीं असेटती ईजा
जिंदगी खुद
लिटवा बन चुकी है
नहीं बोलते लोग
इजा, बाज्यू
दाज्यू, बड़ बाज्यू
काकज्यू,
सब के सब
लुप्त से लगते हैं
बहुत कुछ बदला है
इन दिनों
पहाड़ में भी
धीरे धीरे
विकास के साथ
खोकले
बड़ बोले होते पहाड़
कभी रूठते कभी हँसते और अपने ही भार से
धँसते पहाड़
बहुत कुछ बोल देती थीं
अब तो इनमें
खुर्दरापन है ही नहीं
वो आग
जो वर्षो पहले
जलाती थीं
घर के चूल्हे
हाथ का हथिन्डा
वो कुल्हाड़ी का बिंडा
हल और हलभाणी
वो बल्द की घाँड़ी
वो रामी वो बौराणी
टांडी भांडी
सब स्तब्ध है
खर्क की धुरानी में ध्वांर खा रही है।
इन नरम हाथों को
इनकी जरूरत अब कहाँ
अब तो पोशे की
दुर्गन्ध
दूध के गिलास तक नहीं आती
अब आँगन के किनारे माल्टा, नारंगी, कहाँ
सीमेंट से बूझ दिये गए है दुले
अन्दर ही अन्दर
घुट रही है
दूब और चलमोड़ी
स्याप, मूसे, छीपाड़े, ग्वाण
ये सब तो
अब हम खुद बन चुके हैं
भीड़ों में
घास नहीं उगती
उगती हैं
मन की दूरियाँ
भीड़े बाँट रही हैं हमको
घर की
देहलियों में ऐपण
नकली चिपकने लगे हैं
तुलसी एक डिब्बे में सिमट गयी है
जैसे बूढ़ापा एक कमरे में
पड़ोस से धिनाली का पैना
अब नहीं चलता
दूध बिकता है
गांव का गाँव में
अब आने बाणे
नहीं सुनाती आमा
सुनाये भी किसे
नाती मस्त है
शिनचेन, डोरेमोन
मोटू पतलू के माया जाल में
अब हुक्का लिए
बूबू नहीं लगाते धात
और फटकार
लिटवा नहीं असेटती ईजा
जिंदगी खुद
लिटवा बन चुकी है
नहीं बोलते लोग
इजा, बाज्यू
दाज्यू, बड़ बाज्यू
काकज्यू,
सब के सब
लुप्त से लगते हैं
बहुत कुछ बदला है
इन दिनों
पहाड़ में भी
धीरे धीरे
विकास के साथ
खोकले
बड़ बोले होते पहाड़
कभी रूठते कभी हँसते और अपने ही भार से
धँसते पहाड़
जड़ें
आओ
जम चुके
महानगरों में रम चुके
दम खम दिखा चुके
लेखनी वीरो
अब तो आ जाओ
बंद कमरों से बाहर
जम चुके
महानगरों में रम चुके
दम खम दिखा चुके
लेखनी वीरो
अब तो आ जाओ
बंद कमरों से बाहर
जिसे लिखते हो
उसे जीने के लिए
जो खोया है
उसे पाने के लिए
आँसुओं को लिखना छोड़
आंसुओं को जीने लिए
आओ हकीकत को
परखने के लिए
उसे जीने के लिए
जो खोया है
उसे पाने के लिए
आँसुओं को लिखना छोड़
आंसुओं को जीने लिए
आओ हकीकत को
परखने के लिए
कभी उन झोपड़ियों की तरफ भी
आओ जो टपकती हैं
कभी बारिस
कभी धूप में
जहाँ लड़ती है जिंदगी, जिंदगी से
जहाँ लहू की कीमत
लहू जितनी नहीं
देखो कभी आकर
लहू के रँग और भी होते है यहाँ
आओ जो टपकती हैं
कभी बारिस
कभी धूप में
जहाँ लड़ती है जिंदगी, जिंदगी से
जहाँ लहू की कीमत
लहू जितनी नहीं
देखो कभी आकर
लहू के रँग और भी होते है यहाँ
कभी आओ उन दर्रो के पार
जहाँ से दिखता है
दूसरा आसमान
दुसरी ज़मीं
जहाँ लगी हैं तोपें तेरे और मेरे लिए
बँटे हैं दिल और दिमाग
बांटी गयी है सोच
आओ कलम भी साथ लाना
जहाँ से दिखता है
दूसरा आसमान
दुसरी ज़मीं
जहाँ लगी हैं तोपें तेरे और मेरे लिए
बँटे हैं दिल और दिमाग
बांटी गयी है सोच
आओ कलम भी साथ लाना
निकलो कभी किसान के साथ
किसान बन कर
उन उजड़ चुके पौधों की सिसकती
बालियों को देखो
उन बागों के पास जाओ
जो खो चुके हैं
अपने फलों को
किसान बन कर
उन उजड़ चुके पौधों की सिसकती
बालियों को देखो
उन बागों के पास जाओ
जो खो चुके हैं
अपने फलों को
आओ अपने कैमरों को साथ लाना
उन स्टूडियो से
जहाँ सब कृत्रिम है
कभी फ्लेश मार कर देखो
कैमरा भी रो जायेगा
प्रकृति की विद्रूपता पर
कभी निहारो पहाड़ों को
पहाड़ आकर
कितना मुश्किल है पहाड़ होना
उन स्टूडियो से
जहाँ सब कृत्रिम है
कभी फ्लेश मार कर देखो
कैमरा भी रो जायेगा
प्रकृति की विद्रूपता पर
कभी निहारो पहाड़ों को
पहाड़ आकर
कितना मुश्किल है पहाड़ होना
आओ कविता यहाँ जिन्दा है
संघर्ष में, आँखों में, हाथों में
खुद बोलती है
आँसू बहाती है
और मुस्कुराती भी है
तैयार है
आलोचनाओं के लिए
बड़ी मजबूत है
चला लो अपनी कलम रूपी घन
कहानी कहने को नहीं
जीने को है
जीना है तब आना
गढ़ने को नहीं
संघर्ष में, आँखों में, हाथों में
खुद बोलती है
आँसू बहाती है
और मुस्कुराती भी है
तैयार है
आलोचनाओं के लिए
बड़ी मजबूत है
चला लो अपनी कलम रूपी घन
कहानी कहने को नहीं
जीने को है
जीना है तब आना
गढ़ने को नहीं
बहुत कुछ है
जो बंद कमरों से बाहर आना चाहिए
दिलों के द्वार
खुलने चाहिए
आँखों से नदिया बहनी चाहिए
ह्रदय पिघलना चाहिए
स्वांसों को हवाओं में घुलना चाहिए
आओ अगर चाहते हो
असल में कालजयी बनना
तो काल से लड़ना होगा
लड़ने के लिए मैदान में आना ही होगा
बाहर निकलना ही होगा
जो बंद कमरों से बाहर आना चाहिए
दिलों के द्वार
खुलने चाहिए
आँखों से नदिया बहनी चाहिए
ह्रदय पिघलना चाहिए
स्वांसों को हवाओं में घुलना चाहिए
आओ अगर चाहते हो
असल में कालजयी बनना
तो काल से लड़ना होगा
लड़ने के लिए मैदान में आना ही होगा
बाहर निकलना ही होगा
खुले कैदखाने
इन खुले बगीचों
के खुले तोरण द्वारों
के पीछे
जहाँ कैद हैं
परिन्दे भी
आसमान भी जकड़ा सा है
धरती मचलती है
सब को सजा दे रखी हो जैसे
यहाँ किसी को हाथ हिलाने
पाँव फैलाने की
इजाजत नहीं
उस आम की कातर आँखों को देखा था
जो शायद कह रहीं थीं
अरे मुझे अपाहिज मत बनाओ
उस सदाबहार का जो हस्र
किया था
उस बड़ी-बड़ी आँखों वाले
कैँची चलाते माली ने
बोला था साहब
इसको इससे ज्यादा फैलने न दीहें हम
जा सारो शो ख़राब कर डेत है
सदाबहार रुआँसा सा खड़ा
छोटे बच्चे की तरह सहता रहा
गर्दन झुकाये
कुछ कहे तो
गर्दन ही कट जाय
दूब जो अपनी सौत से परेशान
हर लॉन की जो थी शान
आज हर कोई खींचत है कान
कहीं किसी कोने से आवाज आयी
अरे हमहुँ हैं
मुड़ के देखा
रात की रानी कराह रही थी
अपनी खुशबु को भूल चुकी सी लगी
सब कुछ
था तो चकाचक
पर वो मुझे बाग़ कम
कैदखाना ज्यादा लगा
के खुले तोरण द्वारों
के पीछे
जहाँ कैद हैं
परिन्दे भी
आसमान भी जकड़ा सा है
धरती मचलती है
सब को सजा दे रखी हो जैसे
यहाँ किसी को हाथ हिलाने
पाँव फैलाने की
इजाजत नहीं
उस आम की कातर आँखों को देखा था
जो शायद कह रहीं थीं
अरे मुझे अपाहिज मत बनाओ
उस सदाबहार का जो हस्र
किया था
उस बड़ी-बड़ी आँखों वाले
कैँची चलाते माली ने
बोला था साहब
इसको इससे ज्यादा फैलने न दीहें हम
जा सारो शो ख़राब कर डेत है
सदाबहार रुआँसा सा खड़ा
छोटे बच्चे की तरह सहता रहा
गर्दन झुकाये
कुछ कहे तो
गर्दन ही कट जाय
दूब जो अपनी सौत से परेशान
हर लॉन की जो थी शान
आज हर कोई खींचत है कान
कहीं किसी कोने से आवाज आयी
अरे हमहुँ हैं
मुड़ के देखा
रात की रानी कराह रही थी
अपनी खुशबु को भूल चुकी सी लगी
सब कुछ
था तो चकाचक
पर वो मुझे बाग़ कम
कैदखाना ज्यादा लगा
शब्द लौटे
शब्द लौटे हैं
अपनी सार्थकता के साथ
साथ में ले आये हैं
मात्राएँ
अर्द्ध और पूर्ण विराम
एक नहीं चार विराम
सम्बोधन किया है
आज उत्तम पुरुष ने
प्रथम पुरुष को
मध्यम तो बस माध्यम बना है
शब्द को लाने का
वचन दिया है पूरे होशो हावास में
एक वचन नहीं
बहुवचन
कर्ता बना है बाराती
उस बारात का
जिसमें बर नारायण शब्द है
क्रिया वह वधू है
जो बर माला लिए खड़ी है
कर्ता खड़ा मुस्कुरा रहा है
कर्ता के पीछे छतरी लिए
खड़े है कर्म जी
विशेषण प्रविशेषण नाच रहे है
स्वर व्यंजनों की लय पर
क्रिया सजी धजी निहार रहीं हैं
कर्ता को
अव्यय आज व्यय होने की
सम्भावना तलाश रहा है
समास बांध रहा है
अंचल ग्रंथि
संज्ञा सर्वनाम गा रहे हैं गीत
मंडप के
सन्धि होने को है
स्वर और व्यंजन की
खुश हैं सारे बाराती
क्रिया जो आज उनके पाले में आयी है
स्वर को पा व्यंजन
आज पूर्ण हुआ
शब्द लौटे हैं
अपनी सार्थकता के साथ
साथ में ले आये हैं
मात्राएँ
अर्द्ध और पूर्ण विराम
एक नहीं चार विराम
सम्बोधन किया है
आज उत्तम पुरुष ने
प्रथम पुरुष को
मध्यम तो बस माध्यम बना है
शब्द को लाने का
वचन दिया है पूरे होशो हावास में
एक वचन नहीं
बहुवचन
कर्ता बना है बाराती
उस बारात का
जिसमें बर नारायण शब्द है
क्रिया वह वधू है
जो बर माला लिए खड़ी है
कर्ता खड़ा मुस्कुरा रहा है
कर्ता के पीछे छतरी लिए
खड़े है कर्म जी
विशेषण प्रविशेषण नाच रहे है
स्वर व्यंजनों की लय पर
क्रिया सजी धजी निहार रहीं हैं
कर्ता को
अव्यय आज व्यय होने की
सम्भावना तलाश रहा है
समास बांध रहा है
अंचल ग्रंथि
संज्ञा सर्वनाम गा रहे हैं गीत
मंडप के
सन्धि होने को है
स्वर और व्यंजन की
खुश हैं सारे बाराती
क्रिया जो आज उनके पाले में आयी है
स्वर को पा व्यंजन
आज पूर्ण हुआ
शब्द लौटे हैं
कैमरे
ईटों से पटी सड़कें
कैमरे की एक आँख
संवाददाता की तिरछी नजर
देख रहा हूँ
मैं भी
पिछले कुछ दिनों से
उस बुद्धू बक्से के माध्यम से
जो बोल रहा है
रटी रटाई
छटी छटाई
कुछ बातें
सच है
बहुत कुछ खोया
खोने वालों ने
जो शायद अभी न मिले
हाँ बाद में
मिल सकता है
उन इतिहास के पन्नों में
जब आएगा फिर दोबारा
और हम भूल चुके होंगे
फिर पलटेंगे
उन त्रासदी के रक्त से सने
पन्ने जो शायद
तब जिन्दा हो जाएँ
चीखें चिल्लाएं
और तब भी कोई नहीं होगा सुनने वाला
जैसे आज नहीं है
कैमरे की एक आँख
संवाददाता की तिरछी नजर
देख रहा हूँ
मैं भी
पिछले कुछ दिनों से
उस बुद्धू बक्से के माध्यम से
जो बोल रहा है
रटी रटाई
छटी छटाई
कुछ बातें
सच है
बहुत कुछ खोया
खोने वालों ने
जो शायद अभी न मिले
हाँ बाद में
मिल सकता है
उन इतिहास के पन्नों में
जब आएगा फिर दोबारा
और हम भूल चुके होंगे
फिर पलटेंगे
उन त्रासदी के रक्त से सने
पन्ने जो शायद
तब जिन्दा हो जाएँ
चीखें चिल्लाएं
और तब भी कोई नहीं होगा सुनने वाला
जैसे आज नहीं है
मैं कैसा पहाड़ी?
मैं कैसे कह सकता हूँ कि
मैं पहाड़ी हूँ
मैंने कभी पहाड़ को सुना ही नहीं
जाना ही नहीं
उन पाहनों के दर्द को समझा ही नहीं
जो सम्हाले हुए हैं
अपने कन्धों पर हम सबको
हम जिसके काँधे पर हैं
उसी के कान मरोड़ते फिरते हैं
फिर भी मौन है पहाड़
क्योकि वो तो पहाड़ है
जिसका दिल भी पहाड़ सा विस्तृत
ऊँचाइयाँ लिए हुए है
उन गहराइयों को जीने का साहस
बस पहाड़ को है
मुझ जैसे पहाड़ी को नहीं
पहाड़ सुखद हो
बस यही कैसे हो सकता है
उन दरकती चट्टानों के दर्द को
सुनने और देखने का जज्बा
मुझमें नहीं तो
और किसमें होगा
पहाड़ रोता है
खुद के लिए नहीं
खुद से बिछुड़े लोगों के लिए
उन बंद पडी बाखलियों के लिए
उन सांकलों के लिए
जिन्हें अब खोलने की जरूरत ही नहीं है
वो खुल चुकी हैं
दशकों के इन्तजार के बाद
घास भी जो अब आँगनों में खेलने लगी है
स्वच्छंद होकर
छतों के पाथर जो बोलते थे
धूँए के गुबार से
जो लेते थे महक
भाटिया, दुबका ,चिडक्वानि
माड़े,रौटी की
आज खिसक रहे हैं
सिसक रहे हैं
पथरा से गए हैं
इजा की मुस्कान अब नहीं देख पाते।
अब आँगन के पाथर भी
नहीं नाचते नहीं गाते
झोड़े ,चांचरी ,भगनौले
बैरे ,बग्वाल के के गीत
अब नहीं है
बाखली में वो प्रीत
अब दाज्यू ,बाज्यू
बुबज्यू,सङ्गज्यु,मिज्यु
के मायने बदल गए है
अब नहीं होतीं अठखेलियां
मलगुं और तलगुं में
मैं यहीं रहता हूँ इनके बीच
फिर भी सुन नहीं पाता
इनके मन की टीस
तो मैं कैसा पहाड़ी
मैं पहाड़ी हूँ
मैंने कभी पहाड़ को सुना ही नहीं
जाना ही नहीं
उन पाहनों के दर्द को समझा ही नहीं
जो सम्हाले हुए हैं
अपने कन्धों पर हम सबको
हम जिसके काँधे पर हैं
उसी के कान मरोड़ते फिरते हैं
फिर भी मौन है पहाड़
क्योकि वो तो पहाड़ है
जिसका दिल भी पहाड़ सा विस्तृत
ऊँचाइयाँ लिए हुए है
उन गहराइयों को जीने का साहस
बस पहाड़ को है
मुझ जैसे पहाड़ी को नहीं
पहाड़ सुखद हो
बस यही कैसे हो सकता है
उन दरकती चट्टानों के दर्द को
सुनने और देखने का जज्बा
मुझमें नहीं तो
और किसमें होगा
पहाड़ रोता है
खुद के लिए नहीं
खुद से बिछुड़े लोगों के लिए
उन बंद पडी बाखलियों के लिए
उन सांकलों के लिए
जिन्हें अब खोलने की जरूरत ही नहीं है
वो खुल चुकी हैं
दशकों के इन्तजार के बाद
घास भी जो अब आँगनों में खेलने लगी है
स्वच्छंद होकर
छतों के पाथर जो बोलते थे
धूँए के गुबार से
जो लेते थे महक
भाटिया, दुबका ,चिडक्वानि
माड़े,रौटी की
आज खिसक रहे हैं
सिसक रहे हैं
पथरा से गए हैं
इजा की मुस्कान अब नहीं देख पाते।
अब आँगन के पाथर भी
नहीं नाचते नहीं गाते
झोड़े ,चांचरी ,भगनौले
बैरे ,बग्वाल के के गीत
अब नहीं है
बाखली में वो प्रीत
अब दाज्यू ,बाज्यू
बुबज्यू,सङ्गज्यु,मिज्यु
के मायने बदल गए है
अब नहीं होतीं अठखेलियां
मलगुं और तलगुं में
मैं यहीं रहता हूँ इनके बीच
फिर भी सुन नहीं पाता
इनके मन की टीस
तो मैं कैसा पहाड़ी
ये मैं नहीं कह रहा
प्यासे हैं कुंए
प्यासी हैं नदियाँ
ये 2050 बोल रहा है
मैं नहीं
प्यासी हैं नदियाँ
ये 2050 बोल रहा है
मैं नहीं
हिमालय में उग आयी है घास
सूख गए हैं सोते
लटक गए हैं झरने
गाड़ गधेरे
मौन हो चले हैं
देखो ना कितने स्मार्ट हो चले हैं
ये मैं नहीं
2050 बोल रहा है
सूख गए हैं सोते
लटक गए हैं झरने
गाड़ गधेरे
मौन हो चले हैं
देखो ना कितने स्मार्ट हो चले हैं
ये मैं नहीं
2050 बोल रहा है
हो रहा है युद्ध
आकाश और जमीन के बीच
मशीन और मानव के बीच
सूक्ष्म और स्थूल के बीच
न कोई जीता है
न कोई हारा है
बस युद्ध हुआ है
बस धुंवा उठा है
सुना है
पश्चिम में चीख रहे हैं लोग और भोग
ये मैं नहीं
2050 बोल रहा है
आकाश और जमीन के बीच
मशीन और मानव के बीच
सूक्ष्म और स्थूल के बीच
न कोई जीता है
न कोई हारा है
बस युद्ध हुआ है
बस धुंवा उठा है
सुना है
पश्चिम में चीख रहे हैं लोग और भोग
ये मैं नहीं
2050 बोल रहा है
उड़ रहे हैं जहाज
पंछी के पर काट लिए हैं
उसी से सीख कर
उसी को सता रहे हैं
रोबोट
एक भस्मासुर
भाग रहा है देखो
साफ्टवेयर इंजीनियर
हार्डवेयर से डर कर
त्राहि-त्राहि
ये मैं नहीं
2050 कह रहा है
पंछी के पर काट लिए हैं
उसी से सीख कर
उसी को सता रहे हैं
रोबोट
एक भस्मासुर
भाग रहा है देखो
साफ्टवेयर इंजीनियर
हार्डवेयर से डर कर
त्राहि-त्राहि
ये मैं नहीं
2050 कह रहा है
एक मंथन हुआ है
जिसमें से निकले हैं
जाति और सम्प्रदाय
अमृत की चाह में निकल पड़े हैं
दिग्विजय को
अब समन्दर लाल है
और नदियाँ नीलीं
आदमी का रंग क्या होगा???
जिसमें से निकले हैं
जाति और सम्प्रदाय
अमृत की चाह में निकल पड़े हैं
दिग्विजय को
अब समन्दर लाल है
और नदियाँ नीलीं
आदमी का रंग क्या होगा???
सम्पर्क
मोबाईल
- 09690772783
(इस पोस्ट में प्रयुक्त
पेंटिंग्स वरिष्ठ कवि विजेन्द्र जी की हैं.)






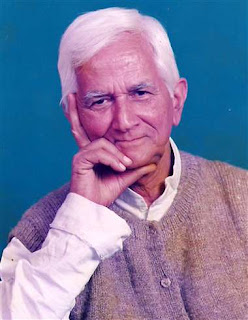


आभार सन्तोष सर का महेश सर का और पहली बार का मित्रो प्रतिक्रिया जरूर दें ।
जवाब देंहटाएंबहुत अच्छी कविताएं गिरीश चन्द्र जी।बधाई।
जवाब देंहटाएं