पंकज चतुर्वेदी की कहानी ‘जाड़ा’
पंकज चतुर्वेदी को हम लोग
उस कवि के रूप में जानते हैं जो छोटी-छोटी कविताओं में बहुत चुटीले अंदाज में अपनी
बातें कह डालने का हुनर रखते हैं। उनके यहाँ भाषा और शिल्प में भी एक अलगाव दिखाई पड़ता है। पंकज
ने एक कहानी लिखी है, जो ‘वागर्थ’ के एक अंक में प्रकाशित भी हुई है। इस कहानी में भी पंकज का यह अंदाजे-बयां महसूस किया जा सकता है। ‘पहली बार’ के
पाठकों के लिए हम इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं पंकज चतुर्वेदी
की पहली कहानी ‘जाड़ा’।
जाड़ा
(कवि मंगलेश डबराल के
लिए)
पंकज चतुर्वेदी
इस बार ठंड इतनी थी, जितनी उत्तर भारत के
मैदानी इलाक़ों में आम तौर पर नहीं पड़ती थी। मैं उसकी दहशत में साँस लेता था। हवाएँ
बहुत सर्द और कँटीली थीं। मेरे पास जाड़े की बहुत सारी यादें थीं, लेकिन ऐसी कोई याद नहीं
थी, जिसमें
वह दुश्मन की तरह पेश आया हो। धूप अक्सर नहीं निकलती थी और शाम से ही कुहरा छाया
रहता था। मैं जब भी बाहर जाता, मुझे लोग उसमें छायाओं
की तरह डोलते दिखते और गाड़ियों की बजाए उनकी धुँधली हेडलाइटें नज़र आतीं। अख़बारों
से पता चलता था कि रेलगाड़ियाँ घंटों देरी से चल रही हैं और कई तो चल ही नहीं रही
हैं। बच्चों के स्कूल बंद थे और लोग कुछ सहमे हुए-से और शाइस्ता हो गये थे और न
जाने क्यों लगता था कि वे उतने वाचाल और सक्रिय नहीं हैं, जितने अमूमन रहते हैं।
मुझे एक दुकानदार ने बताया कि उसके पिता कहते हैं कि इससे भी अधिक जाड़ा सन् बासठ
में पड़ा था, जब
भारत-चीन युद्ध हुआ था। तब चिड़ियाँ ठंड से अकड़ कर पेड़ों से गिर पड़ती थीं और सुबह
जब झाड़ू लगायी जाती थी, वे
मरी मिलती थीं। मुझे याद आया कि बूढ़े, ग़रीब और बीमार लोगों के
लिए यह बहुत सख़्त मौसम है और गाँवों में हेमंत को मृत्यु की ऋतु माना जाता है। सन्
बासठ तक तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर उसके बाद मुझे यक़ीन
है कि ऐसा जाड़ा पड़ा ज़रूर होगा, लेकिन मुझे उसकी स्मृति
नहीं है, क्योंकि
तब मेरी उम्र कम थी। उम्र अधिक होने से जाड़ा अधिक लगता है - जिससे भी मैंने पूछा, वह इस समीकरण से सहमत
था।
इन्हीं दिनों मुझे एक काम से दिल्ली जाना पड़ा, तो वहाँ भी सब लोग यही कह रहे थे कि जाड़ा बहुत है। वे इसे एक दुख की तरह बयान कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि वे दरअसल ख़ुश हैं। इसकी पहली वजह तो यह थी कि उनके पास कहने के लिए एक ठोस बात थी। एक नयी बात। दूसरे, जाड़ा ज़्यादा होने के लिए किसी सरकार या आदमी को गुनहगार नहीं ठहराया जा सकता था और उससे कुढ़ा नहीं जा सकता था। यह एक दुख था, जो अहैतुक था। अगर आपके पास आग के साधन हों, कुछ न करने की छूट देने वाली सम्पन्नता या जवानी जैसी कोई चीज़, तो इसे 'सेलेब्रेट' भी किया जा सकता था।
मैंने एक कवि से कहा कि
जाड़ा ज़्यादा पड़े, तो
मुझे उससे कोई दिक़्क़त नहीं है; लेकिन मैं यही ताज्जुब
किया करता हूँ कि वह इतना नाराज़ और हमलावर क्यों है। उसने मुझे इसका कारण बताया कि
इस बार बारिश ठीक से नहीं हुई, इस लिए ज़मीन में नमी
नहीं है। उसने स्मृति और स्वप्न और सचाई को मानो मिलाते हुए एक निराशाजनक बात कही
कि धूप सारी पहाड़ों में चली गयी है और यहाँ सिर्फ़ ठंड रह गयी है। फिर उसने मुझ से
पूछा कि तुम जो कपड़े पहने हो, उनमें तुम्हें ठंड तो
नहीं लग रही? उस
वक़्त वह कविता से इतनी दूर और जीवन के इतने क़रीब था कि मेरे 'नहीं' कहने के बावजूद उसने
मेरी जैकेट को छू कर देखा, यह
अनुमान करने के लिए कि वह भरोसेमंद है या नहीं।
तीसरे दिन मैंने अपने
शहर के लिए रात की ट्रेन पकड़ी और उसने मुझे छह घंटे विलम्ब से पहुँचाया। दिन में
ग्यारह बजे के आस-पास गाड़ी जब स्टेशन से लगने वाली थी, मैं बड़ी बेसब्री से
खिड़की के बाहर देख रहा था। पर वहाँ वैसा ही कुहरा और धुँधलका था, जैसा मैं छोड़ कर गया
था। पटरी के किनारे बनी झोपड़ियों से धुआँ उठ रहा था। सामने बैठे यात्री से मैंने
कहा कि आधुनिकता और विकास के इतने वर्षों बाद भी यह धुआँ भोजन का संकेत है। उस गाड़ी
में पैंट्री कार नहीं थी। इसलिए वह बहुत दिल से मुस्कराया। तभी उसका फ़ोन आ गया, जिस पर कोई उसे बता रहा
था कि रात का तापमान दो डिग्री से भी कुछ नीचे गिर गया था।
खिचड़ी के दिन तक जाड़ा
उसी तरह पड़ता रहा। फिर दो-तीन दिन कुछ धूप निकली, तो लोगों को लगा कि अब
वह चला जायेगा। मैं एक रिश्तेदार के घर गया, तो मैंने यही बात रखी
कि जाड़ा अब शायद चला जायेगा। वह गाँव की ज़िंदगी से, खेती-किसानी से जुड़े
हुए इंसान थे। इसलिए चिंतित हो कर बोले, गेहूँ के लिए यह अच्छा
नहीं होगा। उसका पौधा बहुत नाज़ुक होता है, इसलिए होली तक जाड़े को
कम ही सही बने रहना चाहिए और इस समय तो एक बारिश होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेतों में नमी
नहीं है।
और सचमुच एक-दो दिन बाद
बारिश हुई और दो-तीन दिन तक थोड़ी-थोड़ी होती रही। जैसे वह गेहूँ के लिए ही हुई थी।
जाड़ा फिर लौट आया। पूरी शान से। पर मुझे लगा कि वह रहने नहीं आया है, सिर्फ़ यह जताने आया है
कि मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊँगा। तुम्हारी सुविधा के लिए मैं यह नहीं करूँगा कि
गेहूँ का ख़याल न रखूँ। मुझे गेहूँ से बहुत रश्क हुआ। रश्क मुझे अपने अपार्टमेंट के
बूढ़े चौकीदार से भी कम नहीं था, जो महँगाई के इस ज़माने
में भी पता नहीं कहाँ से लकड़ी का एक बड़ा कुंदा ले आता था और रात में उसकी आग तापता
था। वैसे मैं भी हीटर जला कर देर रात तक और कभी-कभी सुबह तक भी पढ़ता-लिखता था, पर हीटर में वह बात
कहाँ, जो
कुंदे की आग में है।
रोज़ मैं इस उम्मीद से
उठता था कि आज धूप निकली होगी। पर उसके दर्शन मुहाल थे। एक दिन मैं काफ़ी देर से
जगा, तो
मैंने उसी उम्मीद से माँ से पूछा, बाहर मौसम कैसा है? उन्होंने कहा, ओदा है। इससे जाड़े की
मेरी दहशत कम तो नहीं हुई, पर
शब्द का जैसा अनूठा इस्तेमाल उन्होंने किया था, उससे मुझे एक गरमाहट का
एहसास हुआ।
संपर्क :
हिंदी विभाग,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म.प्र.)—470003
मोबाइल-09425614005



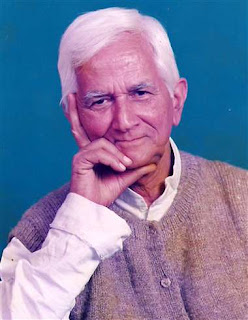


टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें